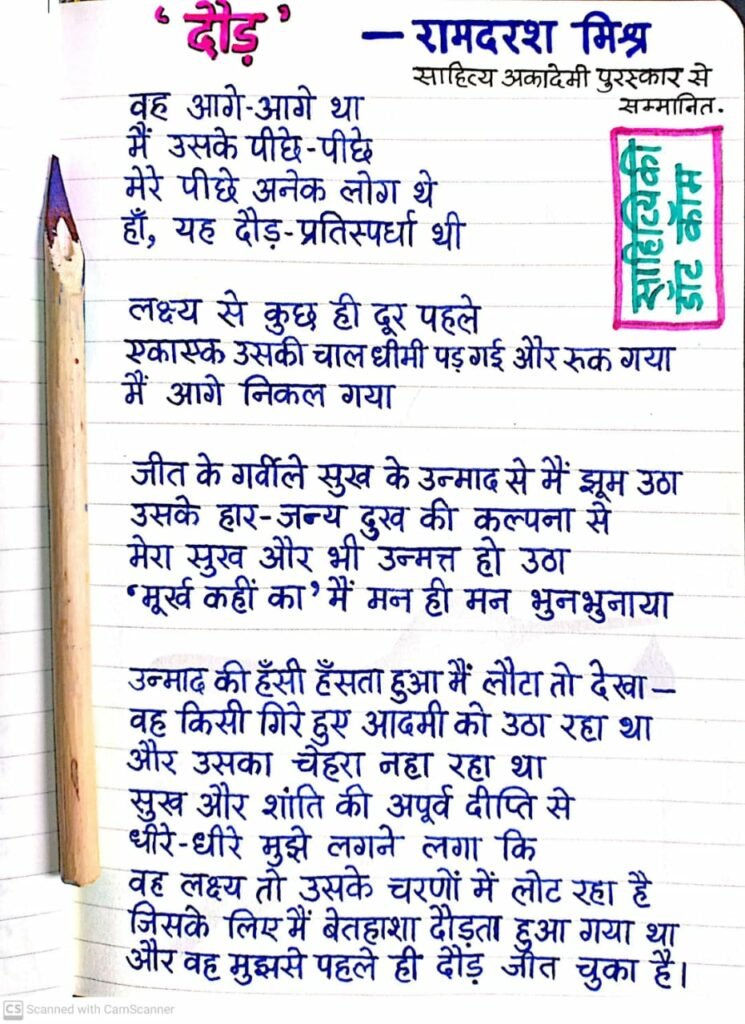यह एक सांस्कृतिक विडंबना ही मानी जाएगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एक सामान्य हिंदी भाषी व्यक्ति का अपने साहित्य और उसके लेखक से भावनात्मक संबंध आज से कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण था। हिंदी भाषा केवल विचारों का माध्यम नहीं, स्वाधीन चेतना का प्रतीक थी और इस अर्थ में हमारे उन समस्त अनुभवों का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे हम व्यापक रूप से भारतीय संस्कृति का नाम देते हैं।
यदि हिंदी की यह भूमिका पिछले वर्षों में धूमिल पड़ गयी है, तो इसके कारणों का विश्लेषण करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य बन जाता है।
प्रायः कहा जाता है कि भारत के अनेक भाषाओ में विभाजित होने से उसके साहित्य का स्वर और स्वरूप उस रूप में अखंडित समग्रता प्राप्त नहीं कर पाता, जितना हम यूरोपीय देशों के एक-भाषी ‘मोनोलिथिक’ साहित्यों में देख पाते हैं। मैं इस आरोप को नितांत सारहीन पाता हूं। यह सही है कि भारतीय भाषाओं की विकास-यात्रा एक-दूसरे से काफी भिन्न रही है। मैं आज उनके उतार-चढ़ाव के विभिन्न कारणों में नहीं जाना चाहूंगा। यह स्पष्ट है कि हर भाषा अनेक दिशाओं से प्रभाव ग्रहण करती हुई अपनी पहचान, अपना विशिष्ट चरित्र गढ़ती है, किंतु कुछ महत्त्वपूर्ण तत्त्व ऐसे भी हैं, जो भारतीय भाषाओं को, उनके वैशिष्ट्य के बावजूद, एक बड़ी सांस्कृतिक अस्मिता में एकसूत्रित भी करते हैं। यह सही है कि कालान्तर से हर भारतीय भाषा को अधिक लचीला, बहुमुखी और समृद्ध बनाने में स्थानीय बोलियों— dilects, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं की भी महत्त्वपूर्ण देन रही। किंतु जहां तक भारतीय भाषाओं के मूल सांस्कृतिक संस्कारों का प्रश्न है, उन्हें सुगठित करने में संस्कृत का योगदान मेरी दृष्टि से उतना ही केंद्रीय महत्त्व रखता है, जितना एक समय में लातिन और ग्रीक भाषाओं ने यूरोपीय देशों के जातीय संस्कारों को निर्मित करने में सक्रिय भूमिका अदा की थी। अंतर यदि था, तो इतना ही कि जब मध्यकाल के समाप्त होने से पूर्व यूरोप में लातिन-ग्रीक भाषाओं के स्रोत सूखने लगे थे, वहां चिंतन, तत्त्वज्ञान और दर्शन के क्षेत्रों में संस्कृत जीवंत माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पोषित करती रही। विभिन्न भाषाओं के भीतर एक ही सांस्कृतिक धारा प्रवहमान होती रही। यह वह मुख्य कारण है कि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां होते हुए भी उनके परस्पर संबंध और सौहार्द का स्नेह बंधन कभी ढीला और कमजोर नहीं पड़ा। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बहुत संवेदनशील शब्दों में ‘अनेक में एक’ की इस अद्भुत भाषाई परंपरा को रेखांकित करते हुए कहा है, ‘हमारे देश ने हजारों वर्ष पहले भाषा की समस्या हल कर दी थी।’ हिमालय से लेकर सेतुबंध तक सारे भारतवर्ष में धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा आदि विषयों की भाषा कुछ सौ वर्ष पहले तक एक ही रही है। यह भाषा संस्कृत रही है। भारतवर्ष का जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ उत्तम है, वह इस भाषा के भंडार में संचित किया गया है। जितनी दूर तक इतिहास हमें पीछे ठेल कर ले जा सकता है, उतनी दूर तक इस भाषा के सिवा हमारा दूसरा कोई सहारा दिखायी नहीं देता।
यह केवल भावोच्छ्वास नहीं है, जब आचार्य आगे चल कर कहते हैं, ‘मैं नहीं जानता कि संसार के दूसरे देश में इतने काल तक इतनी दूरी तक व्याप्त इतने उत्तम मस्तिष्क में विचरण करनेवाली कोई भाषा है या नहीं, शायद नहीं है।“ यह अकारण नहीं था कि उन्नीसवीं शती के मध्य में जब अंग्रेजी शासकों ने भारतीय मानस को औपनिवेशिक ढांचे में ढालने का बीड़ा उठाया, तो मैकाले के एक सहधर्मी अफसर ने कहा था कि भारतीय मस्तिष्क को पश्चिमी संस्कृति में दीक्षित करने के रास्ते में उनके सामने दो बडे़ अवरोध—संस्कृत भाषा और ब्राह्मणों का बौद्धिक वर्चस्व है। यह क्या आंखें खोल देनेवाला सत्य नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साठ वर्ष बाद आज का भारतीय एलीट वर्ग अपनी ‘क्रांतिकारी’ शब्दावली में वही बात दुहरा रहा है, जो दो सौ वर्ष पूर्व स्कूलों के अंग्रेज इंस्पेक्टर ने कही थी?
सच तो यह है कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इन दो पाटों के बीच हुआ था। एक ओर औपनिवेशिक सत्ता का राष्ट्रविरोधी अभियान, जो 1857 के विद्रोह के बाद अधिक तीव्र और आक्रामक हुआ था, दूसरी ओर भारत की जातीय संस्थाओं, शिक्षा पद्धति और परंपरागत आर्थिक और आध्यात्मिक आधारों का अवसान, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय मानस में एक विचित्र प्रकार की शून्यता और क्षोभ का संचार हुआ था। औपनिवेशिक निराशा और विषाद के ये लक्षण और उन्हें नंगी आंखों से देखने का साहस—दोनों ही तत्त्व हम भारतेंदु युग के अनेक लेखकों में देख सकते हैं। हिंदी भाषा का संघर्ष तेजी से जर्जरित होते सांस्कृतिक स्रोतों के बीच अपनी जातीय अस्मिता को प्रतिष्ठित करना था, जिसमें परंपरा के प्रति लगााव उतना ही गहरा था, जितना उसे आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाने का आग्रह। इसके लिए हिन्दी ने दो रास्तों को चुना, जो ऊपर से परस्पर विरोधी जान पड़ते थे, किंतु जो वास्तव में एक-दूसरे के पूरक थे।
पहला रास्ता संस्कृति के उन समस्त तत्त्वों को अपने भीतर समाहित करना था, जिसे विदेशी शासन ने एक-एक करके जातीय जीवन से उन्मूलित करने का प्रयास किया था, दूसरा रास्ता अपने को उन रूढ़ियों, बंधनों और अंधविश्वासों से मुक्त करवाना था, जो आधुनिक संचेतना को अवरुद्ध करते थे। यह उल्लेखनीय है कि हिंदी भाषी प्रदेश में खड़ी बोली के विकास के पीछे जो ऐतिहासिक बाध्यता थी, उसे ये दोनों रास्ते एक-दूसरे से मिलकर मूर्तिमान करते थे।
हिंदी साहित्य और खड़ी बोली ने जिस साहस और सूझ-बूझ के साथ इन दो प्रतिरोधी धाराओं को अपने भीतर समन्वित किया, यह कोई आसान काम नहीं था। यह एक तरह से नंगी तलवार पर चलना था। आधुनिक युग के तथाकथित ‘सेक्युलर’ तकाजों को पूरा करते हुए भी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण रख पाना, विशेष कर उस कठिन समय में, जब विदेशी सत्ता सभ्यता के अपने पुनीत अभियान में भारतीय मनीषा को उसके ‘बर्बर, जंगली संस्कारों’ से उबारने के लिए जी-जान से जुटी थी।
आज जब ‘सभ्यताओं के द्वंद्व’ की बात की जाती है, तो अक्सर यह भुला दिया जाता है, कि इस द्वंद्व के विषैले लक्षण तो तीन सौ वर्ष पूर्व ही दिखायी देने लगे थे, जब समृद्धि और सफलता के दर्पोन्माद में पश्चिमी सभ्यताओं ने यूरोप के बाहर फैली संस्कृतियों को विध्वंस करना आरंभ किया था। भारतीय सभ्यता का प्रभुत्व पश्चिम की आँखों में सब से अधिक चुनौतीपूर्ण था। इसलिए नहीं कि वह सभ्यता अपने सातत्य में सबसे अधिक दीर्घकालीन और प्राचीन थी, बल्कि इसलिए कि उसने मानव संस्कृति के हर क्षेत्र में— दर्शन, तत्त्वचिंतन, आध्यात्मिक और धार्मिक अंतर्दृष्टियों, न्याय, शासन, शिक्षा और भाषा विज्ञान, विविध कलाओं की साधनाओं, नाट्यशास्त्रा आदि में एक संपूर्ण जीवन दृष्टि का अन्वेषण किया था। स्पष्ट ही यूरोपीय सभ्यता के प्रचार में पांच हजार वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता ऐतिहासिक चोटों और घावों के बावजूद सबसे अधिक खतरनाक अवरोध उपस्थित करती थी। यह आकस्मिक नहीं था, कि भारतीय सभ्यता की इस विपुल और समृद्ध धरोहर ने हिंदी के बहुमुखी चरित्र को बनाने में ऐसा योगदान दिया था, कि वह साहित्य की एक व्यापक, सम्पन्न और स्वावलंबी भाषा बन सकी।
यहां यह जोड़ना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हिंदी ने अपना वर्तमान राष्ट्रीय चरित्र बिना किसी ऐतिहासिक बाधाओं अथवा राजनीतिक तनावों से मुठभेड़ किये बिना अर्जित कर लिया था। इसके पीछे संघर्ष की जटिल भूमिका थी। शिक्षा और ज्ञान की समस्त भारतीय संस्थाओं और स्रोतों को, जो अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत के गांवों और शहरों में मौजूद थीं, किस तरह उत्तरोत्तर नष्ट किया गया। यह हमारे औपनिवेशिक अतीत की दारुण गाथा है, जिसका विशद, विस्तृत विश्लेषण भारतीय इतिहासकार श्री धर्मपाल ने अपनी पुस्तकों में किया है। मद्रास, बंगाल और महाराष्ट्र में गांवों की सहकारी पाठशालाओं द्वारा संस्कृत और क्षेत्राीय भाषाओं में समस्त वर्गों, वर्णों, और संप्रदायों के बच्चों को भारतीय ज्ञान-विज्ञान में कैसे दीक्षित किया जाता था, इसका परिचय पहली बार हमें इन पुस्तकों में दिये आंकड़ों से मिलता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि भारत की शिक्षा पद्धति पर अंग्रेजी का आरोपण सिर्फ एक भाषाई संकट न हो, समूची सांस्कृतिक परंपरा के संहार की दुर्घटना बनी थी। हिंदी भाषाई प्रांतों में स्थिति और अधिक बदतर थी। विदेशी सत्ता ने अपनी कूटनीति से समूचे जातीय जीवन में प्रयुक्त होनेवाली हिंदी की खड़ी बोली को शासकीय ढांचे से अलग कर रखा था। सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी या उर्दू-फारसी का व्यवहार होता था। उर्दू के सहज भारतीय संस्कारों को नष्ट करके उसे फारसी के रंग में ढालने का प्रयास किया जा रहा था। इस तरह के कृत्रिम भाषाई विभाजन ने कालान्तर में सांप्रदायिक रूप धारण किया जो अंततः देश के विभाजन का कारण भी बना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय में बहुत सावधानी से किसी देश के भाषाई और जातीय अंतर्संबंधों का विवेचन किया था। उन्हीं के शब्दों में, ”किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की सांस्कृतिक परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती।” इस संदर्भ में वह जो आगे कहते हैं, मेरी दृष्टि में वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उस समय में था, जब शुक्ल जी लिख रहे थे, ”जिस प्रकार हिंदीपन निकाल-निकाल कर एक विदेशी ढांचे की भाषा खड़ी करने का क्रमबद्ध इतिहास है, उसी तरह हिंदी को दूर रखने के घोर प्रयत्नों का भी खासा इतिहास है, जो उस समय से शुरू होता है, जब देश का पूरा शासन अंग्रेजों के हाथ में आया।”
आप देखेंगे, आरंभ से ही हिंदी का दायरा कभी इतना संकीर्ण नहीं रहा कि वह केवल एक प्रादेशिक साहित्य का भाषाई माध्यम बन कर अपने को समेट ले। उसका कर्मक्षेत्र इससे कहीं अधिक व्यापक रहा है। जिन औपनिवेशिक कारणों से उसमें निखार आया, वहां उसके लिए यह नैतिक दायित्व बन गया कि वह देश की घोर निराशापूर्ण दरिद्रता को अनदेखा न करके भारतीय मनुष्य के खोये हुए आत्मविश्वास को पुनः जाग्रत कर सके। भारतेन्दु युग के गद्यकारों—विशेषकर बालमुकुंद गुप्त, प्रतापनारायण मिश्र, और सबसे अधिक स्वयं भारतेंदु हरिशचंद्र की रचनाओं में इस आत्मविश्वास की उगती हुई नयी चमक दिखाई देती है। यह हिन्दी गद्य के उत्थान, ताजगी और ऊर्जा का ऐसा चरण था, जहाँ भारतीय संस्कृति पर होनेवाले उत्तरोत्तर बढ़ते आक्रमणों का सामना किया गया था। पहली बार खड़ी बोली में रचे हिंदी साहित्य का स्वायत्त चरित्र उजागर हुआ था। हिंदी के आत्मबोध की शुरूआत धार्मिक परंपरा और संस्कारों से कटकर पश्चिम की तथाकथित आधुनिकता की नकल करने से उत्पन्न नहीं हुई थी, जैसा हम बंगाल नवजागरण के कतिपय बुद्धिजीवियों में देखते हैं। दूसरी तरफ इसमें अतीत की अंधी पूजा भी नहीं थी। दोनों अतियों के बीच हिंदी की रचनात्मक मेधा एक तीव्र आलोचनात्मक चेतना के भीतर से प्रस्फुटित हुई थी। किंतु यहां हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जरूरी नहीं, जो भाषाएं ऐतिहासिक चुनौतियों के उत्तर में एक तरह का सांस्कृतिक दायित्व अपने ऊपर ओढ़ती हैं, उनका सृजनात्मक साहित्य कलात्मक रूप से भी सशक्त हो। इतिहास में किसी जाति के आत्मबोध का क्षण महत्त्वपूर्ण है, किंतु जन्म लेने के बाद वह तुरंत ही साहित्यिक रचनाओं में अवतरित नहीं हो जाता। उसके लिए मनुष्य के स्वायत्त व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अनिवार्य होता है, जिसे बनने में समय लगता है।
साहित्य में किसी ‘नये’ के आगमन की आहट सुनना एक बात है, उसका कविता या कहानी में कलात्मक सौष्ठव के साथ रूपांतरित होना बिलकुल दूसरी बात है। आज जब हम भारतेंदु युग की ऐतिहासिक देन की बात करते हैं, तो उन आत्म-निबंधों और लेखों की ओर ध्यान अधिक जाता है, जहां हिंदी गद्य की क्रिटिकल चेतना सीधे बाह्य परिस्थितियों के आघातों को व्यक्त करती थी, जो भारतीय संस्कृति पर हो रहे थे, पर हमें उन अंदरूनी संश्लिष्ट परिवर्तनों का अधिक पता नहीं चलता, जो स्वयं व्यक्ति के भीतर हो रहे थे—जिससे अनुभूति-जगत् की बदलती हुई बनावट का पता चल सके।
यह नहीं कि कला और साहित्य में बाहरी परिस्थितियों का कोई महत्त्व नहीं होता, पर उतना ही जितना वे माध्यम से मनुष्य के मानस में होनेवाली हलचलों, परिवर्तनों और नये उन्मेषों को उभासित कर सकें। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इक्का-दुक्का उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा। बंगाल के नवजागरण के दिनों में उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में जो धुंआधार सैद्धांतिक वाद-विवाद हो रहे थे—भारतीय परंपरा और पश्चिमी आधुनिकता के बीच, ब्रह्म समाज के एकेश्वरवाद और धर्म की बहुल दैवी आस्थाओं के बीच—यह एक ऐसी आत्ममंथन की सांस्कृतिक वार्ता थी जिनके प्रमुख प्रतिनिधि राजा राममोहन राय, बंकिमचंद्र, केशवचंद्र सेन, विवेकानंद आदि मनीषी साधक थे। उल्लेखनीय बात यह है कि नवजागरण की यह वार्ता सिर्फ इतिहास के पन्नों पर एक ‘बौद्धिक आंदोलन’ के रूप में अंकित हो कर सिमट जाती, यदि उनका पुंजीभूत प्रतिफलन हमें रवींद्रनाथ के उपन्यास ‘गोरा’ में न दिखाई देता। यह उपन्यास कलात्मक रूप से इसलिए उत्कृष्ट नहीं है, कि वह सिर्फ सैद्धांतिक बहसों का एक जीवंत दस्तावेज है(जो वह है भी), किंतु इसलिए है, कि वह भारतीय नवजागरण के समस्त अंतर-विरोधी तत्त्वों के संश्लिष्ट सम्मिश्रण से उत्पन्न भी हुआ है और पूरी समग्रता से अपनी औपन्यासिक संरचना में प्रतिबिंबित भी करता है। इसी तरह भारतेंदु युग के निबंधात्मक गद्य की व्यंग्यात्मकता और अवसाद अंततः प्रेमचंद की कथाकृतियोंमें अपने समय का अतिक्रमण करती हुई आज भी हमें इतना उद्वेलित कर पाती हैं। यह बात टाॅल्स्टाॅय के उपन्यास ‘युद्ध और शांति’ जैसे एपिक उपन्यास पर और भी अधिक सटीक ढंग से लागू होती है, जो रूस पर नेपोलियन के आक्रमण के पचास वर्ष बाद लिखा गया था, ताकि बीच के अंतराल में रूसी मानसिकता के भीतर जो उथलपुथल हुई थी—उन्हें लेकर लेखक अधिक गहरी निस्संग वस्तुपरकता के साथ ‘रूसी आत्मा’के मर्म को उद्घाटित कर सके।
इन सब उदाहरणों को देने के पीछे मेरा आशय इतना है कि जिन बाहरी परिस्थितियों के संघर्षण से किसी जाति का चरित्र गठन होता है, वे जब तक अपनी पैठ मनुष्य के अनूभूति क्षेत्र की आंतरिकता में नहीं कर लेते, तब तक उनका कलात्मक रूप, कविता या उपन्यास में पूरी उत्कटता से प्रकट नहीं हो सकता। इसके साथ यह भी सच है कि एक बार कलात्मक अभिव्यक्ति पा लेने के बाद वह किसी सामाजिक या ऐतिहासिक व्याख्याओं की तुलना में कहीं अधिक गहरी समग्रता के साथ संवेदनशील और बहुआयामी बना देने में समर्थ होता है।
मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाषा विचारों, विश्वासों और सिद्धांतों को प्रकट करने का माध्यम ही नहीं होती बल्कि उसमें एक जाति सांस्कृतिक बिंब, ऐतिहासिक स्मृतियों और पारंपरिक संस्कारों के मूल स्वर भी अनुगुंजित होते हैं। बहुत पहले आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिम के ‘ओरिएंटलिस्ट’ विद्वानों की व्याख्याओं पर व्यंग्य करते हुए कहा था कि ‘उन्होंने भारत की प्राचीन दर्शन, धर्मशास्त्रों और तत्त्व ज्ञान की पुस्तकों के बीज-शब्दों एवं प्रत्ययों के जो अनुवाद किये हैं, वे सिर्फ भ्रमों की धुंध पैदा करते हैं। इसका सीधा-सा कारण यह है, कि वे इन प्रत्ययों के सांस्कृतिक संदर्भ समझने में नितांत विफल रहे हैं। सच तो यह है कि इन अनुवादों को अस्वीकार करके ही इन ग्रंथों के मूल सत्य को जाना जा सकता है।’
यह उल्लेखनीय है कि भारतीय भाषाओं के जो सांस्कृतिक प्रत्यय यूरोपीय मानस के लिए इतने पराये और भ्रांतिमूलक हो जाते हैं, वे ही भारतीय साहित्य को एक समान जातीय संदर्भ प्रदान करते हैं। भारतीय साहित्य भले ही भिन्न भाषाओं में रचा जाता हो, उसके रचनात्मक स्रोत वेद, उपनिषदों के आध्यात्मिक प्रत्ययों और रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में संगृहित स्मृतियों में ही निहित हैं, जिसके कारण एक भारतीय भाषा में लिखी कविता और कहानी बिना किसी भूल या भ्रांति के दूसरी भाषा में इतनी सुगमता से कायाकल्पित हो जाती है। यह तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं, कुछ वर्ष पहले ‘गोरा’ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ते हुए मुझे वह उपन्यास बहुत बोझिल और बनावटी जान पड़ा था…मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई थी कि रवि बाबू जैसा लेखक ऐसी कमजोर कृति कैसे रच सकता था। किंतु कुछ अंतराल के बाद जब सौभाग्य से इसी उपन्यास का हिंदी अनुवाद पढ़ने को मिला, जो संयोगवश अज्ञेय ने किया था, तो अनायास उस पुस्तक के बारे में न केवल मेरी शंकाएं दूर हो गयीं, बल्कि वह मुझे—जैसा मैं पहले कह चुका हूं—बंगााल नवजागरण का सबसे सशक्त प्रतिनिधि कला-कृति जान पड़ा, जहां पहली बार भारतीय मनुष्य की स्वाघीन चेतना से साक्षात्कार होता है। ऐसा किस किस तरह संभव हो सका? इसका सीधा-सा उत्तर यह है, कि हिंदी अनुवाद में वे समस्त सांस्कृतिक संदर्भ अपनी समूची प्राणवत्ता के साथ अवतरित हुए थे, जैसा उनका प्रयोग बंगला की मूल भाषा में हुआ था। उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद में जो बहसें इतनी बोझिल और सूखी जान पड़ती थीं, वही हिंदी में एक पुरातन सभ्यता के बीच होनेवाले वैचारिक आलोड़न को इतनी जीवंत नाटकीयता और अर्थवत्ता प्रदान करती थीं।
मैं यहां इस बात पर इसलिए भी जोर डालना चाहूंगा कि हिंदी के वर्तमान साहित्य को—उस पर होने वाले समस्त पश्चिमी प्रभावों के बावजूद—हजारों वर्षों से चले इन सांस्कृतिक संदर्भों से काट कर नहीं देखा जा सकता। यही नहीं, मैं कुछ आगे बढ़ कर यह भी जोड़ना चाहूंगा कि पश्चिमी साहित्य और संस्कृति का प्रभाव हमारी सृजनात्मक ऊर्जा को समृद्ध और व्यापक बनाने में उस सीमा तक उपयोगी हो सकते हैं, जिस सीमा तक हमारे साहित्य की घारा अपने परंपरागत स्रोतों से अनवरत प्रेरणा-शक्ति अर्जित करती है। यदि आज हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य की अमर कृतियां—कामायनी, गोदान, शेखर, त्यागपत्र, राम की शक्तिपूजा, मैला आंचल, अंधा युग आदि हमारे भावबोध को कहीं इतने गहरे तक आलोड़ित करती हैं, तो इसलिए कि भक्ति काल के कवियों की भांति उन्होंने हमारे भारतीय मानस के परंपरागत अंतर्संबंधों को एक नये पैटर्न में पुनः संयोजित करने का प्रयास किया, ताकि हम भारतीय मनुष्य की छवि को अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख सकें।
यदि कोई मुझ से पूछे कि भारतीय संस्कृति के मर्म को कौन सा बीज शब्द सटीक ढंग से व्यक्त करता है तो मैं नितांत संशयहीन भाव से उसे ‘अंतर्संबंधों की अंतहीन शृंखला’ का नाम दे सकता हूं। एक ऐसी शृंखला, जिसकी कड़ियां एक जैसी रहती हैं, किंतु उनके आपसी संबंध हमेशा बदलते रहते हैं। सातत्य के बीच होनेवाले परिवर्तन और परिवर्तनों के बीच अक्षुण्ण रहनेवाला सातत्य। संस्कृति का यह मर्म भारतीय दर्शन, तत्त्वज्ञान और आध्यात्मिक अन्वेषण में तो प्रकट होता ही है, किंतु साहित्य में उसका सबसे प्रत्यक्ष और प्रमाणित रूप दिखाई देता है। आत्म की अनात्म से जुड़ने की मर्मांतक आकांक्षा भारतीय महाकाव्यों में जितनी उत्कटता से उद्घाटित होती है, वही कालांतर में भक्ति काव्य की गहन अंतर्दृष्टि और आधुनिक काल की हिंदी साहित्यिक संचेतना में दिखाई देती है। यदि महाभारत में मनुष्य की नैसर्गिक प्रकृति के अंधेरे-उजाले पक्ष दिखाई देते हैं, तो रामायण में उसकी सामाजिक मर्यादाओं के पारिवारिक अंतर्विरोध प्रकट होते हैं। स्वभावगत नैसर्गिकता और नैतिक मर्यादाओं को जोड़नेवाली कड़ी ‘धर्म’ की अवधारणा में अभिव्यक्त होती है, जो परंपरागत नैतिकता और आदिम आकांक्षाओं—दोनों से ऊपर है और दोनों को परिशोधित भी करती है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय समाज में धर्म की यह चालक शक्ति किसी सूत्रा, सिद्धांत या लगे-बंधे फार्मूले में नहीं निरूपित की जा सकती…हर स्थिति में उसकी भूमिका एक जैसी नहीं रहती। यह चीज जहां एक तरफ धर्म की अवधारणा को द्विधात्मक (ambiguous) बनाती है, वहाँ उसे खुला छोड़ कर बहुत अर्थीयता प्रदान करती है। महाभारत के महाकाव्य की अभुत कलात्मक शक्ति खास इस बात में निहित है कि किसी कर्म को काले-सफेद, अच्छे-बुरे, उचित-अनुचित के सरलीकृत ढांचों में नहीं वर्गीकृत किया जा सकता। यहाँ तक कि गीता में कृष्ण का संदेश बहुत देर तक स्मृति में नहीं रहता, जिसके कारण ‘धर्म-संकट’ की स्थितियां बार-बार दुहराई जाती हैं, जिनका समाधान हर बार नये ढंग से किया जाता है।
धर्म की गरिमा का प्रभुत्व और उसके अर्थों की बहुलता भारतीय साहित्य को एक अभुत गतिशीलता प्रदान करती है। इससे हमें साहित्य-समय और समय के अंतर्संबंधों का अनूठा सत्य हाथ लगता है। हमें पता चलता है कि ‘साहित्यिक समय’ अपनी गत्यात्मकता में उससे बहुत भिन्न होता है, जिसे हम ‘ऐतिहासिक समय’ मानते आये हैं। ऐतिहासिक घटनाएं समय के प्रवाह में एक बार प्रकट हो कर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती हैं; याद भी रहती हैं, तो विगत का अंग बन कर। इसके विपरीत साहित्य के सत्य का समय से संबंध एक नितांत दूसरे स्तर पर होता है। साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं सुदूर अतीत में रची होने के बावजूद मनुष्य के हर ‘वर्तमान’ में एक नयी प्रासंगिकता लेकर पुनर्जन्म लेती हैं; अतीत में जन्म लेने पर भी वह विगत का अतिक्रमण कर लेती हैं और समय का एक ऐसा शाश्वत ‘स्पेस’ निर्मित करती हैं, जहां हर रचना एक-दूसरे की समकालीन होती है, चाहे उसके जन्म का समय और स्थान कभी भी हो, कहीं भी हो। इसका प्रमुख कारण यह है कि साहित्य का आत्यंतिक संबंध मनुष्य की आंतरिक प्रकृति से होता है, न कि उन सामयिक घटनाओं से जो सतह के ऊपर से गुजर जाती हैं।
मैं यदि साहित्य के इस सर्वविदित सत्य को दुहराने की जरूरत महसूस कर रहा हूं, तो इतिहास या ऐतिहासिक घटनाओं का महत्त्व कम करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भारतीय मनीषा में इतिहास की वह आक्रामक चालक-शक्ति कभी नहीं रही, जैसा हम पश्चिमी संस्कृति में देखते हैं। इतिहास के इस प्रभुत्व के कारण ही मैक्समूलर जैसे ‘ओरिएंटलिस्ट’ विद्वानों ने भारत के अतीत को उसके वर्तमान से इस तरह विभाजित कर दिया, जैसे इन देानों के बीच साहित्य और संस्कृति के कोई संबंध-सूत्र न हों। उनकी दृष्टि में भारत का वर्तमान उसके ‘गौरवपूर्ण’ अतीत का महज एक भ्रष्ट संस्करण मात्रा था, जिसका अपना कोई भविष्य नहीं था, सिवा इसके कि वह यूरोपीय साहित्य और संस्कृति में अपने को ढाल कर स्वयं को अपने अतीत से हमेशा के लिए मुक्त कर सके। अंग्रेजी शासन-तंत्र भारतीय मनीषा में जो फांक अंकित कर गया था, वह आज एक नासूर की तरह कायम है, जिसने उन समस्त स्रोतों को सूखा और बंजर बना कर छोड़ दिया है, जिनसे एक समय में भारतीय साहित्य और भाषाएँ अपनी ऊर्जा का नवीकरण करती थीं।
आधुनिक हिंदी साहित्य—इन अवरोधों के बावजूद—यदि निरंतर अपने को नयी परिस्थितियों में ढालने में समर्थ होता रहा, तो इसके दो प्रमुख कारण मुझे दिखाई देते हैं। दोनों अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे से अंतर्गुम्फित हैं। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का एक वयस्क साहित्यिक भाषा के रूपमें प्रसार—मेरी दृष्टि में एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना थी। शायद ही किन्हीं अन्य भारतीय भाषाओं में इस तरह का ‘भाषाई मोड़’ दिखाई देता है। कौन अनुमान लगा सकता है कि जिस भाषा में आधुनिक हिंदी कहानी और उपन्यास का जन्म और विकास हुआ, वह मुश्किल से डेढ़ सौ वर्ष से अधिक नहीं है। आधुनिक हिन्दी कविता ब्रजभाषा और अवधी से अपने को मुक्त करके एक नितांत नये मुहावरे में, नयी संवेदनाओं, अनुभवों और आकांक्षाओं को व्यक्त करने की शक्ति जुटा पायेगी, यह केवल ऐसी भाषा में संभव हो सकता था, जिसमें बाह्य प्रभावों को अपने में समाहित करने की क्षमता और लचीलापन दोनों ही हों, और यह चीज मुझे उसके विकास के दूसरे कारण की ओर ले जाती है—हिंदी का अपनी प्रादेशिक सीमाओं से ऊपर उठकर ‘भारतीय’ होने की सांस्कृतिक अंतःप्रेरणा, जिसके कारण उसे विदेशी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में सहज रूप से ‘राष्ट्रीय भाषा’ बनने का गौरव प्राप्त हो सका। यह अकारण नहीं कि उस समय दूसरी भाषाओं के शीर्षस्थ साहित्यकार, रवींद्रनाथ ठाकुर, सुब्रह्मण्यम भारती आदि अनेक लेखक हिंदी को राष्ट्रीय अस्मिता और एकता का एक केंद्रीय प्रतीक मानते आये थे।
आज जब हम हिंदी साहित्य के वर्तमान और भविष्य पर विचार कर रहे हैं तो हमें भारतीय मानस के इन तत्त्वों को नहीं भुला देना चाहिए जो समय और इतिहास की खूंटी पर न बंधे होकर संस्कृति की उन अंतःप्रक्रियाओं द्वारा अनुप्राणित होते हैं, जिन्हें युंग जैसे पश्चिम के मनोवैज्ञानिक आदिम या ंतबीमजलचंस तत्त्व कहते हैं—ऐसे प्रागैतिहासिक मिथक और प्रतीक, जो एक जाति के अवचेतन में वास करते हैं – एक संस्कृति के कालातीत अवयव, जो हर युग में बाह्य दबावों का सामना करने के लिए अपने को पुनर्गठित कर लेते हैं। पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में भाषा और साहित्य का गहरा योगदान रहता है। भाषा में उसकी चिरंतनता और साहित्य में उसकी गतिशीलता देखी जा सकती है। यह महज संयोग नहीं था कि जिस भाषा में सत्य, अहिंसा, आत्म, शून्य, मुक्ति जैसे प्रत्यय इतना महत्त्व रखते हैं, वे ही कालांतर में बुद्ध के निर्वाण दर्शन, गांधी के सत्य-आग्रह और अहिंसा-प्रेम, श्री अरविंद की आध्यात्मिक गूढ़ अंतर्दृष्टि में नयी धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक अर्थवत्ता प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य इन दोनों ध्रुवों—एक तरफ परंपरागत प्रतीकों और मूल्यों का सातत्य और दूसरी तरफ परिवर्तनशील मानवीय संवेदनाओं की व्यापकता—के बीच अपना विशिष्ट और बहुमुखी पहचान बना सका था।
यह एक ऐतिहासिक विडंबना ही मानी जायगी कि स्वतंत्राता आंदोलन के ज्वार में हिंदी को जो राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ था, वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद धूमिल पड़ता गया। यह हिंदी का दुर्भाग्य ही नहीं, समूची भारतीय संस्कृति की त्रासदी थी, कि दो सौ वर्षो के दौरान जिस विदेशी सत्ता ने हमारे शिक्षण-अध्ययन और चिंतन के जिन स्वदेशी स्रोतों को इतनी बर्बरता से नष्ट किया था, उन्हें हमारे जातीय जीवन में पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, उलटे हमारी मानसिकता पर राजकीय संस्थाओं और शिक्षा-प्रणाली का आतंककारी प्रभुत्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया, जो एक समय में विदेशी राज्य-सत्ता की प्रशासनिक सुविधाओं के लिए निर्मित की गयी थी, स्वाधीन भारत में पराधीन संस्कृति का यह एक अनुपम उदाहरण था। आधुनिकता के उन्माद के बावजूद हमारे सार्वजनिक जीवन में जो शून्यता, दरिद्रता और दिशाहीनता दिखाई देती है, उसके कारण खोज पाना मुश्किल नहीं है।
एक प्राचीन सभ्यता की प्राणवत्ता उसके सांस्कृतिक प्रतीकों और जीवनदायी आस्थाओं में संचारित होती है, जो एक समय में हमारे चिंतन, सृजन और दैनिक व्यावहारिक जीवन को एक अर्थवत्ता प्रदान करते थे; जब उनकी जीवंत समग्रता खंडित हो कर छोटे-छोटे टुकड़ो में बंट जाती है, परंपरागत संस्कारों के कारण उनकी नामलेवा पूजा तो होती है, किंतु समाज को उससे किसी तरह की सृजनात्मक प्रेरणा अथवा आत्मनिर्भरता की आश्वस्ति प्राप्त नहीं होती। हम अपने ही देश में आत्मनिर्वासित प्राणियों की तरह जीने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। पिछले वर्षों में हमारे जीवन की नैतिक-मर्यादाओं और चिंतन-अध्ययन के स्रोतों पर जिस तरह अंग्रेजी भाषा और शिक्षा का वर्चस्व बढ़ा है, वह इसका स्वयं सटीक प्रमाण है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बहुत अवसाद भरे शब्दों में हमारी सांस्कृतिक दुर्दशा का वर्णन किया है, ”अंग्रेजी भाषा ने संस्कृत का सर्वाधिकार छीन लिया है। आज भारतीय विद्याओं की जैसी विवेचना और विचार अंग्रेजी भाषा में है, उसकी आधी चर्चा का भी दावा कोई भारतीय भाषा नहीं कर सकती। यह हमारी सबसे बड़ी पराजय है। राजनीतिक सत्ता के छिन जाने से हम उतने नतमस्तक नहीं हैं, जितने अपने विचार की, दर्शन की, अध्यात्म की अपनी सर्वस्व भाषा छिन जाने से। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम अपनी ही विद्या को अपनी बोली में न कह सकने के उपहासास्पद अपराधी हैं। यह लज्जा हमारी जातीय है।“
जिसे द्विवेदी जी ने ‘उपहासास्पद अपराध’ कहा है, उसके लिए मेरी दृष्टि में भारतीय संभ्रांत शिक्षित वर्ग सबसे अधिक जवाबदेह रहा है, एक तरफ इस वर्ग को शिक्षा और ज्ञान अर्जित करने की समस्त सुविधाएं प्राप्त हैं, दूसरी ओर वह उन सब कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति उदासीन हैं, जो एक बुद्धिजीवी वर्ग अपने समाज में संपन्न करता है। अपनी और साहित्य की जिन जड़ों से उनके संस्कार पोषित होते हैं, वह धीरे-धीरे उनसे कटता जाता है और एक कृत्रिम परिवेश में रहने लगता है।
‘आत्म-ज्ञान रहित ज्ञान’ का बंजर मरुस्थल, जहां आत्मचेतना के विस्तार की कोई संभावना नहीं। इसका दुष्परिणाम हमारे सामने है…..हमारे हिंदी भाषी समाज में, जिसका गद्य भारतेंदु युग में एक खुली और गहरी आलोचनात्मक मेधा से संपन्न था, आज वहां एक खाली और क्रांतिकारी रेह्टरिक के अलावा किसी तरह की वयस्क और विवेकपूर्ण चेतना नहीं दिखाई देती। हिंदी साहित्य की रचनात्मक संवेदनाएं अपने में इतना समृद्ध होने पर भी केवल एक छोटे वर्ग तक सीमित रह गयी हैं। हिंदी भाषाई समाज की लोक चेतना का विस्तार और परिष्कार करने में उनकी भूमिका नगण्य जान पड़ती है। क्या हम इन दोनों के बीच फैले अंतराल को पाट कर एक व्यापक सांस्कृतिक चेतना में संयोजित कर पाने में सफल हो पायेंगे? आनेवाले समय में हमारे सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है।
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के पूणे, महाराष्ट्र में 16 मार्च 2004 को 56वां अधिवेशन के सभापति के पद से दिए गये भाषण का अंश।)