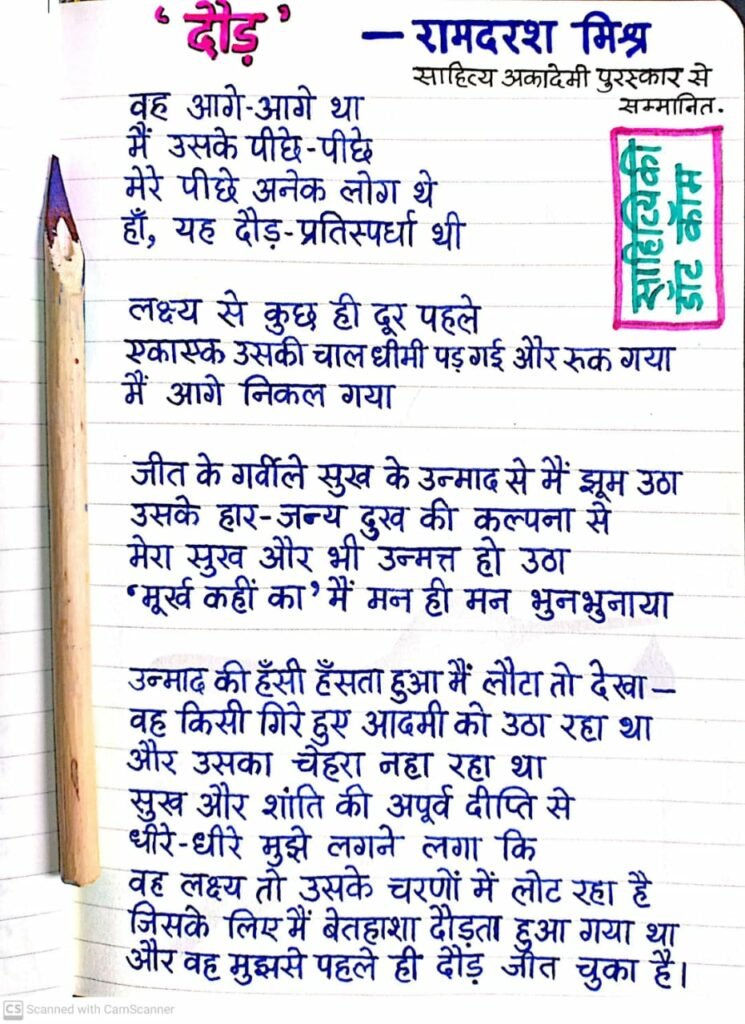राष्ट्र – राज्य की अवधारणा में मुख्य बात है भूमि की पवित्रता का भाव और वहां पर रहने वाली जनता में भावात्मक एकता का भाव। पश्चिम में यह अवधारणा आधुनिक काल के साथ दिखायी देती है। 17 वीं सदी से पहले किसी भी हालत में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत भूमि की पवित्रता और जनता में एकता के भाव की शुरूआत की तिथि तय कर पना लगभग असंभव है। मोटे तौर पर सुदूर अतीत से ही भारत में यह भाव प्रबल रहा है। भारत भूमि का आकर्षण भारतीयों के लिए ही नहीं विदेशियों के लिए भी बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए बेनेडिक्ट एंडरसन जैसे लोग जो राष्ट्र को कल्पित राजनीतिक समुदाय मानते हैं वे पश्चिम के इतिहास के दबाव में दिखाई देते हैं साथ ही ये भी अनयास ही मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिम के राष्ट्रवाद की प्रायः नकल है और पश्चिमी राष्ट्रवाद के जो दुर्गुण हैं वे सब भारतीय राष्ट्रवाद में भी सहजता से ही निहित हैं और पश्चिमी राष्ट्रवाद की आलोचना में जो कुछ कहा जाता है वही सब कुछ भारत के बारे में भी कहा जा सकता है और वह सब कुछ अनिवार्यतः सही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यह इतिहास की विधेयवादी दृष्टि है जिसमें पहले घटने वाली घटना कारण और बाद में घटने वाली घटना कारण मान ली जाती है। चूंकि पश्चिम में राष्ट्रवाद का विकास पहले हुआ और भारत में बाद में इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का मूल पश्चिम में है। जबकि ऐेसा नहीं है। डॉ. एस. आबिद हुसैन ने अपनी पुस्तक भारत की राष्ट्रीय संस्कृति में लिखा है कि भारत का हजारों वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास दर्शाता है कि एकता का सूक्ष्म किंतु मजबूत धागा, जो उसके जीवन की अनंत विविधताओं से होकर जाता है, सत्ता समूहों के जोर देने या दबाव के कारण नहीं बुना गया, बल्कि भविष्य दृष्टाओं की दृष्टि, संतों की चेतना, दार्शनिकों के चिंतन और कवि कलाकारों की कल्पना का परिणाम है और केवल ये ही माध्यम हैं, जिनका राष्ट्रीय एकता को व्यापक, मजबूत और स्थायी बनाने में उपयोग किया जा सकता है।[i] आबिद हुसैन की इस मान्यता के बारे में उपर्युक्त पुस्तक की भूमिका के लेखक मान्य दार्शनिक और शिक्षाविद् डॉ. एस. राधाकृष्णन ने आश्चर्य से देखते हुए लिखा कि यह कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि हमारी सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, जबकि हमारी सांस्कृतिक जड़ें आध्यात्मिक मूल्यों में हैं।[ii] हम देखेंगे कि भारत का राष्ट्रवाद सभ्यतामूलक होने के नाते पश्चिम से अपनी बुनियाद ही नहीं बल्कि रूप और रचना में भी भिन्न है।
फिलहाल तुर्की का उदाहरण। एक समय ता जब तुर्की का आटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था और राष्ट्रवाद की लहर ने केवल ईसाई राष्ट्रों को अलग कर दिया बल्कि इस्लाम के अनुयाई अरब राष्ट्र भी तुर्की से अलग हो गये। अगर राष्ट्रीयता कल्पित सत्य है तो धर्म निरपेक्षता और समाजवाद भी उतने ही कल्पित कहे जा सकते हैं। उसी तरह पाकिस्तान की मांग को भि जो लोग राष्ट्रवाद से प्रेरित मानते हैं या थे वे देख सकते हैं कि पाकिस्तान अपने निर्माण के समय जितना खतरनाक और भयावह था आज सालों बाद उससे ज्यादा भयावह और खतरनाक हो गया है।
जवाहरलाल नेहरू स्वंत्रता आंदोलन के दिनों में देश का भ्रमण करते हुए भारतमाता की जय के नारे लगाते लोगों से पूछते थे कि आप जिस भारत माता की जय का नारा लगाते हैं वह कौन है? पहली बार उनको पश्चिमी उत्तरप्रदेश के एक जाट ने जवाब दिया कि भारतमाता का मतलब है यह धरती माता। तब जवाहरलाल नेहरू ने उसको समझाया कि भारत माता केवल धरती नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं और भारत माता की जय का मतलब यहां के लोगों की जय है।[iii] विष्णु पुराण में भी भारत की भूमि और जनता के संबंध को माता और संतान के मुहावरे में समझाते हुए कहा गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में फैले हुए विस्तृत भूभाग को भारत कहते हैं और यहां पर रहने वाले लोग भारत की संतान हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक राज्य के चार तत्व होते हैं क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। लेकिन नेहरू और विष्णु पुराण दोनों ही भारत के संदर्भ में केवल दो का उल्लेख करते हैं। इसका एक सभ्यतामूलक पक्ष है कि राज्य सरकार केंद्रित होता है और सरकार के लिए संप्रभुता सबसे जरूरी होती है लेकिन सभ्यता या समाज के लिए लोक महत्वपूर्ण होता है और लोक सरकार का मुंह देखकर आगे नहीं बढ़ता बल्कि वह अपनी पारंपरिक शक्ति से आगे बढ़ता है। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्र का एक सत्ता मूलक विमर्श होता है और एक सभ्यतामूलक विमर्श है। और यूरोपीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में यही अंतर है। एक विचारधारा और आंदोलन के रूप में राष्ट्रवाद का विकास एक आधुनिक परिघटना है जिसके मूल में विज्ञान तकनीकि का विकास और औद्योगिक क्रंति के फलस्वरूप यूरोप में एक ही साथ आधुनिकता, राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक साम्राज्यवाद जैसी चीजें देखने को मिलीं। तर्क और मानव को हर चीज का केंद्र मान लेने का नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया को उसके कुपरिणाम भुगतने पड़े और इसने यूरोप के बाहर के देशों को स्वतंत्र समाज से गुलाम उपनिवेश बना दिया और खुद यूरोप में जातीय श्रेष्ठता के अहंकार में विश्वयुद्ध तक लड़े गये और आधुनिक सभ्यता ने पारंपरिक सभ्यताओं को खाने का प्रयास किया।
इसके अलावा मनुष्य की श्रेष्ठता के भाव ने सदियों से चले आ रहे प्रकृति और मानव के संबंध को ध्वस्त कर दिया और मनुष्य के लिए प्रकृति पर विजय पाना ( शोषण करना) जरूरी हो गया। ऐेसा नहीं है कि पारंपरिक सभ्यताओं में मनुष्य को महत्व नहीं दिया गया था। खुद तुलसीदास मनुष्य जन्म को देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताते हैं। लेकिन इसमें मनुष्य ८४ लाख योनियों में से एक योनि मात्र है और मनुष्य होना आत्म विकास का सर्वोत्तम साधन है न कि प्रकृति के शोषण का खुला लाइसेंस। जबकि आधुनिक समाज में मनुष्य के लिए अन्य प्राणियों, पेड़- पौधों और नदियों का दोहन ( शोषण) किया जा सकता है। मनुष्य की यह केंद्रीयता दुनिया के सभी मनुष्यों के लिए समान नहीं है। यह मनुष्य आधुनिक पश्चिमी यूरोप का मनुष्य है जो लोकतांत्रिक और सेक्यलर अर्थात धर्महीन। अतः बाकी मनुष्यों के लिए यही यूरोपीय मनुष्य आदर्श प्राणी है जिसका मतलब है कि विकसित होकर सबको उसी तरह से एक रूप बनना है। इसीलिए गांधीजी ने इस्लामी शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज में आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा था। वस्तुतः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के मूल में दुनिया को लूटने और अपनी श्रेष्ठता कायम करने की भावना थी। जो राष्ट्रवाद यूरोप में संघर्ष का कारण बन गया वही राष्ट्रवाद औपनिवेशिक दासता के शिकार देशों में विदेशी शासन से जूझने की प्रेरणा भी लेकर आया।
१९ वीं सदी जहां यूरोप में राष्ट्रवाद की आंधी कि सदी थी तो २० वीं सदी में यह आंधी एशिया में आई और औपनिवेशिक दासता के बंधन टूट गये।
आधुनिक भारत का हर नेता या चिंतक अपने आप को राष्ट्रवादी कहता था जबकि अंग्रेज भारत को एक राष्ट्र मानने से हमेशा इंकार करते रहे और उनका यह दुराग्रह आजादी के बाद भी प्रेत बनकर भारत को सता रहा है। उनके लिए भारतीय तो भारत के लोहों के लिए एक अन्य संज्ञा मात्र है। एक एंग्लों इंडियन के शब्दों में, भारत को जानने के लिए भूलना होगा कि भारत जैसी कोई चीज है। दूसरी ओर हिंदू राजनीतिज्ञ और देश भक्त भारत को एक राष्ट्र बताने में कभी नहीं चूके और इस पर बराबर बल देते रहे।[iv] उन्होंने यह महसूस किया था कि राष्ट्रीयता का स्वराज के दावे से गहरा संबंध है। वह जानते थे कि १९ वीं सदी के अंत में यह एक मान्य सिद्धांत हो गया था कि एक राष्ट्र के रूप में रहने वाले लोग स्वशासन के अधिकारी हैं और अपनी जनता के लिए स्वशासन की मांग करने वाले किसी भी देशभक्त को यह सिद्ध करना होगा कि वह जनता एक राष्ट्र है।[v] इटली के चिंतक मैजिनी ने राष्ट्रों के स्वशासन के अधिकार का समर्थन किया। लेकिन यूरोप में जो राष्ट्रवाद खड़ा हुआ उसमें एक जाति, धर्म और भाषा जैसी चीजें महत्वपूर्ण थीं। अतः वहां राष्ट्रवाद की दो अनुभूतियां एक साथ काम कर रही थीं पहली यह की अपने समुदाय के लोगों के प्रति अपनाव या लगाव का भाव और दूसरे जो अपने से अलग हैं उनके प्रति अपनत्व विरोधी अनुभूति। चार्ल्स द गाल देशभक्ति और राष्ट्रवाद में अंतर बताते हुए कहते हैं कि जब अपने लोगों के प्रति प्रेम का भाव प्रमुख हो तो देशभक्ति है लेकिन राष्ट्रवाद में दूसरों के प्रति घृणा प्रमुख होती है। पश्चिम में राष्ट्रवाद की आलोचना की एक लंबी परंपरा है जिसमें जार्ज बर्नार्ड शा, अलबर्ट आइंस्टीन और जार्ज आरवेल जैसे लोग प्रमुख हैं। आइंस्टीन तो इसे एक बीमारी ही मानते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की आलोचना का मूल तत्व राष्ट्रवाद के भीतर पल रहा श्रेष्ठता का अहंकार ही था। यूरोप में राष्ट्रवाद की आलोचना की देखा देखी भारत में भी कुछ लोग राष्ट्र वाद की आलोचना करने लगे। वस्तुतः अपनों से प्रेम से ज्यादा दूसरों से घृणा का भाव लोगों को आपस में ज्यादा करीब लाता है और सामाजिक वर्गीकरण और भेदभाव इसके नीचे छिप जाते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसे शब्द तो नेशन और नेशनलिज्म की तर्ज पर आये लेकिन केवल अपना शरीर लेकर। भारत की जनता ने उसमें अपनी तरफ से अपना पारंपरिक अर्थ ही भरा। बेनेडिक्ट ऐंडरसन ने राष्ट्र को कल्पित राजनीतिक समुदाय बताया तो यह बात यूरोपीय राष्ट्रवाद के अर्थ में बिलकुल सही थी लेकिन भारत में भी कुछ लोग राष्ट्रवाद को वैसा ही साबित करने की कोशिश करते हैं। इसे निर्मल वर्मा औपनिवेशिक विस्मृति का सजीव उदाहरण मानते हैं। भारत में विदेशी दासता से मुक्ति पाने की लालसा महज राजनीतिक उद्देश्यों से उत्प्रेरित नहीं थी, उसके पीछे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को विस्मृति के अंधेरे से बाहर लाने की आकांक्षा भी थी। इस दृष्टि से यह यूरोप की आधुनिक राष्ट्रीय सत्ताओं ( नेशन स्टेट्स) की आक्रामक अहंग्रस्त भावना से कुछ अलग थीजिसकी स्थापना अनेक जातियों, नस्लों, और जन भाषाओं को नष्ट करने के बाद ही संभव हुई थी।[vi]
भारत में एकता के राजनीतिक अर्थ उतने गहरे नहीं थे जिसने सांस्कृतिक। हालांकि अंग्रेजों का यह दावा था कि उन्होंने भारत का राजनीतिक एकीकरण किया भले ही आजादी समय भी सैकड़ों रियासतें थी। परन्तु अपने इस कार्य में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को खंडित कर दिया। भारत यूरोपीय अर्थों में न तो तब राष्ट्र था और न आज है और उसे आगे भी वैसा नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त संकल्पनाओं का गहरा रिश्ता देश और काल की अवधारणा से भी है। यूरोप में इतिहास एक रैखिक गति करता हुआ आगे बढ़ रहा है जहां घटनाएं देश और काल के एक निश्चित बिन्दु पर घटित होती हैं जबकि भारत में उसका कोई खास महत्व नहीं रहा है। यूरोप का मनुष्य अपनी केंद्रीयता में पहले अन्य प्राणियों और चीजों से श्रेष्ठ होकर अलग हुआ और उसके बाद उसका अलगाव चर्च से हुआ और एक समय के घोर राष्ट्रवादी लोग आज परिवार से भी अलग होकर कहे के लिए तो ग्लोबल हो चुके हैं लेकिन अपने अंतरतम में वे बिलकुल अकेले हैं। मनुष्य का आत्म निर्वासन विशेष रूप से आधुनिक बोध की देन है। यूरोप में आधुनिकता का आंदोलन एक ऐसे खंडित कालबोध से उत्पन्न हुआ था जिसमें मनुष्य का इतिहासबोध और परंपरा दो स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित हो गये थे।[vii] लेकिन भारत में यह बोध आज भी बहुत व्यापक नहीं हो पाया है तो उसका कारण है भारत में देश, काल और परंपरा का गहरा बोध जहां मनुष्य प्रकृति और भूगोल के बीच एक जीवित संबंध आज भी बना हुआ है। यहां के पहाड़, वृक्ष और नदी अपना निजी व्यक्तित्व और चरित्र रखते हैं जो मनुष्य के लिए आदरणीय हैं। पेड़ से सूखी लकड़ी तो तोड़ी जा सकती है लेकिन नई टहनी तोड़ना पाप है इतना तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी समझता है।
भारत में समग्रता या संलग्नता का बोध बहुत महत्वपूर्ण रहा है और इसीलिए भारत को किसी एक खांचे में फिट करने की कोशिशें कभी सफल नहीं हुईं। भारतीय सभ्यता सनातन परंपरा का एक ऐतिहासिक और जीवंत रूप है और भले ही इसकी शास्त्रीय परंपराओं को नष्ट कर दिया गया हो लेकिन इसकी लोक परंपराएं आज भी जीवित हैं। [viii] भारत को भले ही समुदायों या जातियों का देश माना जाता हो लेकिन ये समुदाय स्वतंत्र होने के बावजूद एक दूसरे से बिलकुल गहराई से जुड़े थे और यह बात केवल समुदायों ही नहीं बल्कि विभिन्न कलाओं, संप्रदायों भाषाओं के मामले में भी सच है। भारतीय जीवन दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हम और वे का विवाद चाह कर भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता और घृणा का स्थायी भाव भारत में कभी जमने नहीं पाया। अपने आत्म का विस्तार भारत में केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं है बल्कि एक सचाई है जिसकी वजह से धर्मांतरण की अवधारणा के लिए भारत में कोई जगह नहीं थी। धर्म व्यक्ति के विकास का मार्ग है न कि समुदाय की संख्या बढ़ाने का माध्यम। यही स्थिति भाषाओं के मामले में भी रही है। भारत एक बहु भाषी समाज रहा है यहां हर आदमी एक से अधिक भाषाएं जानता और प्रयोग करता था। इसलिए राष्ट्र के लिए एक धर्म या एक भाषा के आधार की बात करना निरर्थक है। पृथ्वीराज रासो का कवि चंदबरदाई षट् भाषा पुरानं च कुरानं कथितं मया के विवेक के साथ रचना कर्म में प्रवृत्त होता था। एक सभ्यता का समग्रता बोध – क्या मतलब है इसका? मेरा अभिप्राय अर्थों के उस तंतुजाल, उस टेक्सचर से है, जहां सब धागे एक समूचे जीवन की अर्थव्यवस्था के पैटर्न बुनते हैं। एक का अर्थ दूसरे में खुलता है, दूसरे का अर्थ तीसरे से जुड़ा है – अर्थों की अन्योन्याश्रित व्यवस्था- जिसमें भितर और बाहर का संबंध – मनुष्य की एकीकृत आत्मछवि और बाहरी जगत की विविध अनन्त छवियां एक ही सूत्र में अंतरर्ग्रथित हैं।[ix] भारतीय राष्ट्र ने इस्लामी हमले को सफलता पूर्वक इसलिए झेल लिया क्योंकि वह वैचारिक स्तर पर कोई चुनौती लेकर नहीं आया था और खुद भारत में इस समय विराट लोकजागरण भक्ति आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में चल रहा था। लेकिन जब नई तकनीक और विज्ञान लेकर अंग्रेज आये तो भारत के बुद्धिजीवियों के सामने संकट खड़ा हो गया कि अब क्या करें? हमारा अतीत तो महान रहा है लेकिन आज हम इनके सामने क्या हैं? और यहीं से भारत के गौरवमय अतीत और को साथ लेकर आधुनिक यूरोप की तरह विकास करने की महत्वाकांक्षा ने हमें अपनी चपेट में ले लिया। इस नई वैचारिकी में दो बातें थीं धार्मिक स्तर पर ये सनातन पूजा परंपरा को अंधविश्वास साबित कर रही थी और राजनीतिक तौर पर भारत का एकीकरण और लोकतंत्रीकरण करने लगी। लेकिन दो महापुरूषों ने इसके ये दोनों विषैले दांत उखाड़ दिये। राजाराममोहन राय जहां अंग्रेजी अरबी फारसी और संस्कृत के ज्ञान के साथ इस कथित नवजागरण के अग्रदूत बने जिनका लक्ष्य एकेश्वर वाद की स्थापना और मूर्तिपूजा के विरोध के साथ देश सुधार था। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू पर इनका प्रभाव पड़ा। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो न तो पढ़े लिखे थे और न ही पश्चिम के किसी विचार से परिचित थे उन्होंने न केवल मूर्ति पूजा की बल्कि पूजा के लिए जिस देवी काली को चुना वह आधुनिक नवजागरण की भावना के ठीक विपरीत थी। इतना ही नहीं उन्होंने विभिन्न संप्रदायों की साधना पद्धतियों का अभ्यास करके सिद्ध किया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक ईश्वर एक पूजा पद्धति और एक किताब का दावा हास्यास्पद है। इसके बाद गांधीजी आये और उन्होंने तो अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में अंग्रेजी राज के सबसे मजबूत और धारदार औजार लोकतंत्र की आलोचना करते हुए इंग्लैंड की संसद को बांझ और वेश्या तक कहा। यानी न तो वह रचनात्मक है और न ही उसकी कोई नैतिकता है। खुद गांधीजी धर्म को राजनीति से अलग किये जाने के घोर विरोधी थे। और इस प्रकार गांधीजी ने अंग्रेजी राज के राजनीतिक विषदंत को भी उखाड़ दिया। गांधीजी के लिए भारत और उसकी स्वतंत्रता केवल राजनीतिक चीज नहीं थी। वह एक सभ्यतामूलक चिंता थी जिसमें अंग्रेजी राज और इसकी सभ्यता से घृणा तो थी परंतु अंग्रेजों से नहीं थी। इतना ही नहीं भारत की आजादी की जितनी जल्दी अन्य नेताओं को थी उतनी गांधीजी को नहीं थी।
राजनीति से अलग राष्ट्रवाद से जुड़े एक सवाल को प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में उठाया है। स्कंद गुप्त को ऐतिहासिक रूप से भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने वाले शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने भारत को हूणों के आक्रमण से बचाया था। नाटक के पहले ही दृश्य में स्कंदगुप्त मंच पर आता है और कहता है कि अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन होता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की आजादी का आंदोलन भारत की जनता के स्थानीय राष्ट्रीय और मानवीय अधिकारों के संघर्ष और रक्षा का आंदोलन था ऐेसे में प्रसाद जी जैसे परमदेशभक्त के एक प्रमुखचरित्र के मुंह से यह संवाद क्या ध्वनित करता है ? वस्तुतः यही वह कुंजी है भारत में राष्ट्र के बोध को समझने की जहां सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता से जुड़ा अधिकार बोध( अहंकार) सारहीन है । इसलिए भारतीय राष्ट्र को राजनीतिक दृष्टि से देखने पर कुछ हाथ नहीं आता सिवाय इसके कि भारत ने औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्र बनना शुरू किया है और अभी तक बन नहीं पाया।
भारतीय सभ्यता में अगर अंग्रेज न भी आये होते तो भी राष्ट्रवाद का प्रचार और प्रसार होता। यही असली बात है जिसने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, कबीर गुरू नानक, तुलसीदास से लेकर गुरुगोविंद सिंह तक सबको प्रेरणा दी। अगर ऐेसा न होता तो संतों के अखाड़ों का सैन्यीकरण न होता और 1857 में होनेवाला संग्राम अखिल भारतीय स्तर पर नहीं फैल पाता।आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक आनंदमठ के मूल में संन्यासी विद्रोह ही था। भारतीयता की परिभाषा का प्रश्न भी इसीलिए लगातार उठता रहा है। गाँधीजी ने हिंदुत्व की सहनशील प्रवृत्ति को सत्य की खोज को ही भारतीयता की पहचान मानते हुए कहा कि मूल भावना है जियो और जीने दो। वे कहते हैं कि अगर मुझे हिंदुत्व को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो मैं सिर्फ इतना कहूँगाः अहिंसक तरीके से सत्य की खोज …. हिंदुत्व सत्य का धर्म है। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर को न मानना यहाँ चलता है पर सत्य को न मानना असंभव है।[x]
लेकिन प्रश्न उठता है कि भारत में अगर राष्ट्रवाद का भाव सदियों से रहा है तो उसके स्रोत हमें क्यों नहीं मिलते? वस्तुतः यही असली समस्या है।भारत में जो भी आधिकारिक इतिहास मौजूद है वह पश्चिमी शिक्षा प्राप्त लोगों द्वारा प्रायः अंग्रजी में सत्ता धारी वर्ग की जरूरतों के हिसाब से लिखा गया है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि भारत का निर्माण अंग्रेजों ने किया है, यह किस्सा इतनी दफे दोहराया जा चुका है कि इसमें कुछ- कुछ सचाई लगने लगती है( जैसा कि झूठ को बार- बार दोहराने से उसके सच हो जाने की लोकोक्ति भी बताती है)। लेकिन, निश्चित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के एक समन्वित इकाई होने की अवधारणा कोई नई नहीं है और पिछले हजार वर्षों में अनेक संदर्भों में इसकी चर्चा होती आई है। किसी सम्राट का ( जैसे चंद्रगुप्त या अशोक या अकबर) इलाका कहाँ तक था या कहाँ तक जा सकता था, यह चर्चा तो रही ही है। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के खड़े होने और पसरने – पहुँचने के संदर्भों में भी एक भारत की चर्चा होती रही है।[xi] भारत बहुत लंबे समय से अस्तित्व में रहा है लेकिन उसके अस्तित्व के साक्ष्य तलाशने की प्रक्रिया में दृष्टियों की बड़ी भूमिका रही है। भारत में ऐसा वैदिक काल से ही माना जाता है कि भारत भूमि पवित्र है और यहाँ पर रहने वाले भारत माता की संतान हैं। भूमि की पवित्रता और जनता में भाईचारे की भावना ही राष्ट्र की मुख्य शर्तें रही हैं। ये तत्व भारत में बहुत प्राचीन काल से ही मौजूद रहे हैं जबकि पश्चिम में एक खास समय पर ये भाव प्रकट हुए और आज प्रायः विलुप्त हो चुके हैं। फिर भारत की राष्ट्र के रूप में अवधारणा उतनी विवादित इसलिए रही कि भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत प्रायः शास्त्रीय परंपरा के ग्रंथ ही रहे हैं चाहे वह परंपरा संस्कृत की रही हो या अरबी फारसी की। लेकिन अब जरूरत है कि हम परंपरा के देसी और लोक स्रोतों की ओर देखें तथा उन पर और शोध करें। दूसरी बात सभ्यतामूलक संदर्भ का आयाम भारत को पश्चिम से भिन्न बनाता है जिसमें समस्त अस्तित्व पवित्र और दैवीय माना जाता है। इसलिए भू खंड की पवित्रता और दैवीयता के साथ जनता की एकता का भाव स्वतः सिद्ध है। लेकिन ये तत्व सभ्यतामूलक विमर्श के अंतर्गत आते हैं और हमारे आधुनिक जीवन में लोक परंपरा में मौजूद जीवित सत्य से कट गये हैं और हमारी पहचान के प्रामाणिक सूत्र प्राचीन ग्रंथों में बड़ी मुश्किल से तलाशे जा रहे हैं जबकि हमारा इतिहास एक सभ्यता के रूप में भारतीय जनता की मनोरचना में मौजूद है जरूरत है तो उससे जुड़कर उसे पढ़ने की।
डॉ. विवेकानंद उपाध्याय
[i] आबिद हुसैन, भारत की राष्ट्रीय संस्कृति, पृ.12, नेशनल बुक ट्रस्ट, छठा संस्करण 2003
[ii] डॉ. एस. राधाकृष्णन, भारत की राष्ट्रीय संस्कृति, प्राक्कथन, नेशनल बुक ट्रस्ट, छठा संस्करण 2003
[iii] नेहरू जवाहरलाल, डिस्कवरी आफ इंडिया, पृ. ५३, पेंगुइन बुक्स नई दिल्ली, २००४
[iv] डा. भीमराव अंबेडकर, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पृ. ४७, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली- २००९
[v] वही
[vi] निर्मल वर्मा, पत्थर और बहता पानी, पृ- १०५, वाग्देवी प्रकाशन बीकानेर, २०००
[vii] निर्मल वर्मा, पत्थर और बहता पानी, पृ- ३१, वाग्देवी प्रकाशन बीकानेर, २०००
[viii] अमित शर्मा, हिंद स्वराज की प्रासंगिकता, कौटिल्य प्रकाशन २००५
[ix] निर्मल वर्मा, पत्थर और बहता पानी, पृ- १११, वाग्देवी प्रकाशन बीकानेर, २०००
[x] महात्मा गाँधी, अमर्त्य सेन द्वारा उद्धृत, अतीत का वर्तमान पृ.- 21, ग्रंथ शिल्पी-2002
[xi] अमर्त्य सेन, अतीत का वर्तमान पृ.- 23, ग्रंथ शिल्पी-2002