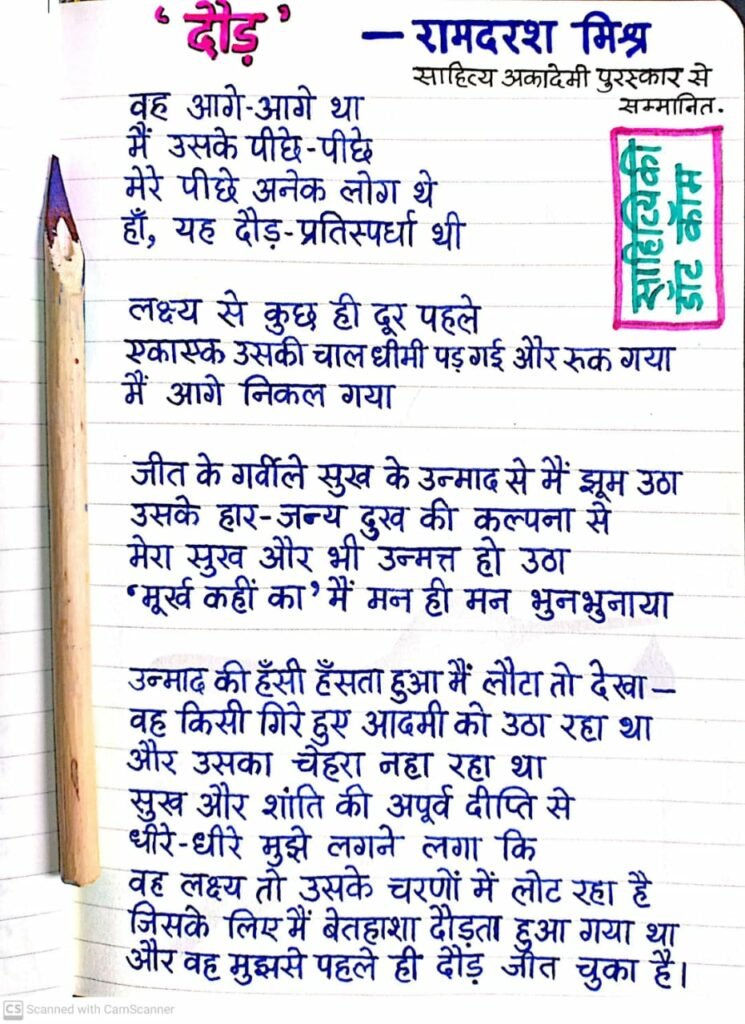सन् 1893 में एनी बेसेंट ने थियोसाफिकल सोसाइटी का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। उन्होंने सन् 1898 में काशी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और हिंदू कन्या विद्यालय की स्थापना की। इसके साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों में शिक्षण संस्थाएँ खोलीं। महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों में भारतीय संस्कृति की शिक्षा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में दी जाती थी। इस सोसाइटी पर अंग्रेजी का भी प्रभाव दिखाई देता है, किन्तु इनकी जो भी प्रचारादि सामग्री छपती, वह अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी होती थी। इस प्रकार हिन्दी-प्रसार को सुअवसर मिला। स्वाधीनता संग्राम के प्रति विशेष लगाव होने के कारण सन् 1918 से सन् 1921 तक उन्होंने दक्षिणी भारत में घूम-घूमकर हिन्दी का प्रचार किया था। उन्होंने हिन्दी का महत्त्व अपनी पुस्तक ‘नेशन बिल्डिंग’ में लिखा है— “हिन्दी जानने वाले आदमी संपूर्ण भारत में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिन्दी बोलने वाले मनुष्य मिल सकते हैं। हिन्दी सीखने का कार्य ऐसा त्याग है, जिसे दक्षिणी भारत के निवासियों को राष्ट्र की एकता के हित में करना चाहिए।”
बेसेंट के उपर्युक्त विचार अप्रत्याशित हैं तथा मन में कौतुहल भी जगाते हैं। हालांकि यह भी सच है की हिंदी के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका का मूल्याङ्कन न के बराबर ही हुआ है। अतएव, प्रस्तुत आलेख में मैं यह कोशिश करूँगा कि उनकी इस भूमिका का एक विस्तृत सामाजिक-राजनैतिक सन्दर्भ में मूल्यांकन कर सकूँ।
पर इससे पहले की मेरी दूसरी बातें आपके ज़ेहन में जायं, मैं चाहता हूँ कि मेरे बोलते रहने तक ये दो ध्वनियाँ आपके अंतस में गूंजती रहें। एक तो वह जो एनी बेसेंट ने भारत से अपने जुड़ाव के बारे में कहा था। वह है— “मैं जितना भारत को प्यार करती हूँ उतना किसी को नहीं …यह मेरी दूसरी मातृभूमि है…” (न्यू इंडिया,1918)
और दूसरी वह जो सरोजिनी नायडू ने एनी बेसेंट के बारे में कहा था— “यदि एनी बेसेंट न होतीं तो गांधी जी भी न हुए होते।”
व्यक्तिगत रूप से मुझे, ऊपर के ये दोनों कथन बेतरह सम्मोहित करते हैं। एक सुखद आश्चर्य से भर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक, मैं एनी बेसेंट के बारे में बस सूचनात्मक ही जानता था। शायद बस इतना कि एक आयरिश अंग्रेजिन जिसने गुलाम भारत में कुछ कार्य किये, सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज बनाया और जिसे अपने जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी मां कहते थे।
पर जैसा कि कहते है न कि वह तो पढ़ो ही जो किसी ने लिखा है, पर वह और ध्यान से पढो जो उसने पढ़ा है। कृष्णमूर्ति मुझे प्रिय है और यह मुझे बहुत बाद में पता चला कि उन्हें एनी बेसेंट को पढना प्रिय था। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ यह भी एक और क्षण था जब मेरी रूचि बेसेंट में बढ़ी।
और मैं उन्हें पढ़ता चला गया। उनके द्वारा किया गया भगवद्गीता का भाष्य तो कई दफे पढ़ गया। पर आज जब उनके बारे में कुछ बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक अजीब संकोच और असमंजस में हूँ। सवाल मेरे सामने बिलकुल साफ़ है कि आखिर नीली आँखों और हिंदुस्तानी सपनों वाली, विदेशी मिटटी और भारतीय मन वाली इस महीयसी को जानने,समझने की दृष्टि क्या हो। क्या राजनैतिक? या एतिहासिक? या दार्शनिक? या थियोसाफिकल? या सोसलिस्ट? या मार्क्सिस्ट? या स्त्रीवादी? या हिंदूवादी? या कुछ और? क्योंकि अपने जीवन में वे इन सब रास्तों से होकर गुजरीं और अंत में अपने आप को सिर्फ सत्यान्वेषी कहा— सत्यान्वेषी, किसी अमूर्त ब्रह्म की नहीं, बल्कि मनुष्यता की, तथा इस तलाश में जिसके पास रौशनी के रूप में कुछ था तो वह बस शुद्ध प्रेम, प्रेम का साम्राज्य था।
इसीलिए मुझे लगता है उनका व्यक्त्तित्व इन वैचारिक चौखटों में नहीं अंटता। वे इनसे परे हैं। शायद एक ऐसी सन्यासिनी, जिसने गुफा छोड़कर स्वयं को समाज में सान दिया। इसलिए चूँकि मैं स्वयं को एक साहित्त्यिक/कवि मानता हूँ अतः मैं उन्हें इसी दृष्टि से देखूँगा अर्थात् एक लेखक की तरह, ताकि उनके जीवन संघर्ष का सर्वांग निरूपण हो सके क्योंकि मूलतः वे भी लेखिका ही थीं। ताज्जुब नहीं कि उन्होंने लगभग ३०० पुस्तकें और पैम्फलेट्स लिखे।
पर कुछ और कहने से पहले मैं आपके सामने एक दृश्य रखता हूँ। एनी बेसेंट तब मात्र ४० साल की थी। वे मार्क्सवादी हो चुकी थीं।1888 में वे लंदन स्कूल बोर्ड के चुनाव में खड़ी हुईं और रिकार्ड मतों से जीतीं।संसदीय चुनाव में तब महिलाएं नहीं खडी हो सकती थीं, पर १८८१ से स्थानीय चुनावों में उन्हें अवसर मिल गया था। जीत की ख़ुशी में उन्होंने अपने बालों में लाल रिबन लगाया और विजय सभा में पहुंची। और उन्होंने पहली घोषणा की— “लंदन में अब कोई बच्चा भूखा नहीं होगा।”
दरअसल, पति से तलाक के बाद एक बच्चे की कस्टडी उन्हें नहीं मिली थी। और अपनी इसी लड़ाई को उन्होंने समाज की लड़ाई बना दिया। और शायद यह, उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी था।
कह सकते हैं कि वे एक संघर्षशील स्त्री थीं, जिसकी चेतना उनमें अनवरत यूं ही बनी रही। बस मंजिलें बदलती गईं।
और वे एक ऐसा ही व्यक्तित्व लेकर भारत आयी थीं। अपने शेष जीवन के कर्म भी उन्होंने यहीं किये। भारत की वजह से वह जानी भी जाती हैं। उनके किये गए कर्मों से हम सब परिचित हैं। उन्होंने एक बेहतरीन स्कूलिंग सिस्टम भारत को दिया। होमरूल आन्दोलन की स्थापना की। थियोसाफिकल चिंतन को विस्तार दिया। कृष्णमूर्ति को नया जन्म देकर विश्व को दिया।
पर भले ही आप सबको अजीब लगे लेकिन यह सच है कि उनके मूल्याङ्कन को लेकर आज मतभेद हैं। और इन मतभेदों की चर्चा जरूरी है क्योंकि यह सांस्कृतिक विमर्शों का जरूरी हिस्सा है। शायद इन मतभेदों की चर्चा कर उन्हें समझने में हमें और भी आसानी हो।
इस लिहाज से अगर आप ध्यान दें तो विशेषकर परतंत्र भारत के समय में, भारत में कर्मरत विदेशी विद्वानों को लेकर वर्तमान भारतीय मेधा के बीच मतभेद बढ़े हैं। एक तो वह वैचारिक ग्रुप है जो उनकी देनों को स्वीकार करता है। भारत की पुनर्संरचना में उनके दिए योगदान को मानता है। पर एक दूसरा वैचारिक ग्रुप भी है, जिसे परम्परावादी कहा जाता है, तथा जो उनकी देनों को अस्वीकार करता है। इस ग्रुप के अनुसार तत्कालीन पश्चिमी चिन्तक,जो भारत में कर्मरत रहे, वे दरअसल अंग्रेजी राज के आवरण थे। वे उसकी निरंकुशता पर पर्दा डालते थे। अंग्रेज मारते थे तो वे सहलाते थे तथा कुल मिलाकर भारत की स्वतंत्रता और पुनर्जागरण के आन्दोलन में उनका कोई योगदान न था।
इन परम्परावादियों में कई हैं पर मैं इस प्रसंग में प्रसिद्ध साहित्यकार निर्मल वर्मा की सोच को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपने लेख ‘भारत और यूरोप: प्रतिश्रुति के क्षेत्र’ में उन्होंने इस मूल्याङ्कन को एक नयी वैचारिक जमीन प्रदान की है। विशेषकर अंग्रेजी साम्राज्य की वृहत्तर व्यूह रचना के छल छद्म को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। उनकी मान्यता है कि पश्चिम सिर्फ लूटने और खोखला करने भारत आया था। यह भ्रम है कि अंग्रेजों के लक्ष्य कल्याणकारी थे। लेकिन वे तब भी भारत की आत्मा को पूरी तरह खंडित न कर सके। हालाँकि उन्होंने भारत के चेहरे को धुंधला और रक्तरंजित जरूर कर दिया। वे लिखते हैं— “पश्चिम, पूरी तरह से भारत को नष्ट न कर सका। हालाँकि उसने उसके आत्म-चित्र को धुंधला जरूर कर दिया। भारत भ्रम से भर उठा। यूरोपीय दृष्टि को वह भले न स्वीकार कर सका, पर जीवन के अपने दृष्टिकोण के प्रति शंकालु अवश्य हो उठा।”
अर्थात् निर्मल वर्मा के मत में पश्चिम ने भारत पर न केवल भौगोलिक वरन सांस्कृतिक हमला भी किया। न केवल बल से वरन बुद्धि से भी भारत को अपने अधीन किया। सेनाओं ने जहाँ शरीर पर अधिकार किया तो वहीं पश्चिमी बुद्धिजीवियों ने भारतीय मेधा और स्मृति को अधिकृत कर लिया। भारत इन्ही पश्चिमी बुद्धिजीवियों की वजह से अपने ही जीवन की समझ के प्रति संभ्रमित हो गया। इसका और परिणाम क्या हुआ, इस पर वे आगे लिखते हैं—“पश्चिम के प्रभाव से भारत में एक छद्म चेतना का उदय हुआ, जिसका गहरा प्रभाव बंगाली भद्र लोक पर पड़ा। उसने इसे बाद में शेष भारत पर लागू करने की कोशिश की।”
यानी निर्मल के कहने का नीचोड़ यह है की ब्रिटिश और पूरा पश्चिम, भारत की बहुस्तरीय गुलामी के प्रोजेक्ट में संलग्न था और पश्चिम के बुद्धिजीवी भी इसमें शामिल थे, जाहिर है स्वयं एनी बेसेंट इनसे अलग कैसे हो सकती थीं। इस प्रसंग में अगर ध्यान दें तो, विशेषकर होमरूल आन्दोलन की असफलता को लेकर बेसेंट पर आरोप भी लगाये जाते हैं। जब तिलक और उनके नेतृत्त्व में यह आन्दोलन अंग्रेजों की खिलाफ निर्णायक हो रहा था तब बेसेंट ने उसे डीफ्यूज करने की कोशिश की। और इस कारण तिलक ने उनका साथ छोड़ दिया। निर्मल के मत में होमरूल को लेकर तिलक ने एक वृहद् संकल्पना की थी तथा उसके समर्थन में एक व्यापक जनाधार भी उभरा था पर बेसेंट ने जिस तरह भीतर से ही उसे कुंद किया वह अकल्पनीय,अजीब और भारत के साथ एक एतिहासिक धोखा था। इसने स्वतंत्रता संघर्ष को और लम्बा खींच दिया।
जाहिर है कि निर्मल इन्हीं सब कारणों के आधार पर कहते हैं कि इन पश्चिमी बुद्धिजीवियों ने अपने चमकीले सिद्धांतों से तत्कालीन भारतीय मेधा के अवचेतन को भी गुलाम बना लिया।
और यह एक सशक्त थियरी है जो विश्वास से परे भी नहीं यदि हम उस समय को ठीक से पढ़े। आप ज़रा १९ वीं सदी के उत्तरार्ध के गुलाम भारत में सक्रिय भारतीय बुद्धिजीवियों के के विचारों पर ध्यान दें। तत्कालीन अधिकांश भारतीय बुद्धिजीवी अंग्रेजी शासन को ‘दैवी विधान’ कहते थे। राजा राम मोहन राय ने कहा— भारतीय बहुत भाग्यशाली हैं की इश्वर ने उन्हें ब्रिटिश राष्ट्र का संरक्षण दिया है। कांग्रेस के संस्थापक सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने कहा— प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए हम सभी इंग्लैण्ड की ओर ही देखते हैं। इंग्लैण्ड ही हमारा राजनैतिक मार्गदर्शक एवं नैतिक शिक्षक है।दादा भाई नौरोजी ने कहा— अंग्रेजी शासन दिव्य है। उसके कई लाभ हैं। गोखले के सर्वेन्ट्स आफ सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को शपथ लेना पड़ता था की ब्रिटिश शासन भारत के लाभ के लिए है।
जाहिर है निर्मल वर्मा की बात को हम हलके में नहीं ले सकते। गुलामी का वह दौर बहुस्तरीय था। इसलिए एनी बेसेंट के किसी भी मूल्याङ्कन से पूर्व हमें हमारी चेतना को झगझोरना भी पड़ेगा। कई सवाल उठाने होंगे,जैसे कहीं वे तत्कालीन साम्राज्यवादी सत्ता की ‘बौद्धिक और नैतिक खोल’ तो नहीं थीं? उनके द्वारा आरम्भ भारतीयशैक्षिक आन्दोलन आखिर कितना भारतीय था या है? कई विद्वानों ने यह भी आरोप लगाये हैं की बेसेंट ने जोशैक्षिक पाठ्यक्रम भारत को दिया वह उसकी जड़ों से बहुत दूर था। क्या यह आरोप सही है ?जाहिर है की यह सारे सवाल हैं जिन पर बहस होती रहेगी, होनी चाहिए।
पर व्यक्तिगत रूप से मैं, एनी बेसेंट के सम्यक मूल्याङ्कन हेतु उन्ही बातों को यहाँ रखूँगा जो उन्हें पढ़कर मैंने महसूस किया है। और सच कहूँ तो इस जमीन पर मैं स्वयं को निर्मल से और अन्य परम्परावादियों से अलग पाता हूँ।
मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ। बेसेंट 1875 में ही कहती हैं— ब्रिटिश शासन ने भारत की आत्मा तक को गरीब बना दिया है।१८७८ में उन्होंने ‘England, India and Afghanistan’में ब्रिटिश शासन की निंदा की। यह पुस्तक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है। यह भारतीय सांस्कृतिक जागरण और स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से एक ‘चमकती हुई किताब’ है। उन्होंने जोर देकर कहा जो पश्चिम द्वारा भारतीयों को सभ्य करने के सिद्धांत के समर्थक हैं, वे अज्ञानी हैं क्योंकि भारत उस समय विश्व सभ्यता का केंद्र था जब पश्चिमी देशों के लोग नग्न जंगली के समान आपस में लड़ते थे।उन्होंने यह भी कहा— “भारत पर ब्रिटिश शासन सभ्य देश पर असभ्य एवं व्यापारियों का शासन है।अंग्रेज लूटेरे हैं। संभवतः इसीलिए आज भी अधिकांश लोग दावे से कहते हैं एनी बेसेंट ने दरअसल भारत की तरफ से ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला विरोध किया था।स्वयं महात्मा गाँधी कहते हैं- ‘उन्होंने भारत को एक गहरी निद्रा से जगाया।”
जाहिर है कि एनी बेसेंट की आवाज एक प्रामाणिक आवाज है जिसे हमें सुनना चाहिए। सुनना इसलिए भी चाहिए कि वे डीक्लास हो चुकी थीं, ईसाइयत के फ्रैंकसटीन से मुक्त हो चुकी थीं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों में इसी राक्षस को खाद पानी डालते वे देख चुकी थीं। आप उन्हें ध्यान से पढ़ें तो स्वतंत्रता के संघर्ष में ईसाइयत का जबरदस्त विरोध करते हुए उनकी आवाज हममें शामिल होती है। अपनी आत्मकथा में वे लिखती हैं—“for centuries the leaders of Christian thought spoke of women as a necessary evil, and that the greatest saints of the Church were those who despised women the most……Against the teachings of eternal torture, of the vicarious atonement, of the infallibility of the Bible, I leveled all the strength of my brain and tongue, and I exposed the history of the Christian Church with unsparing hand, its persecutions, its religious wars, its cruelties, its oppressions.”
ध्यान दें, ईसाईयत के खिलाफ लिखित रूप से यह चुनिन्दा विरोधों में से एक है। अपने व्यक्तिगत जीवन की जटिल और त्रासद श्रृंखलाओं को वे इसाइयत की देन मानती हैं। और उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए उसके प्रति अपनी सम्पूर्ण आस्था को नकार देती हैं। यह उल्लेखनीय है कि वे लिखती हैं—I was a wife and mother, blameless in moral life, with a deep sense of duty and a proud self-respect; it was while I was this that doubt struck me, and while I was in the guarded circle of the home, with no dream of outside work or outside liberty, that I lost all faith in Christianity.
और शायद यही कारण था कि उनका आस्था-व्याकुल धार्मिक मन किसी और जमीन को खोज रहा था। और उन्होंने भारत को चुना। भारत आकर अपने मन की आस्था को वे इस पवित्र मिट्टी से जोडती हैं और सनातन धर्म, संस्कृति से अपने तन मन को जोडती हैं। इसे ही अपनी वैचारिकी में वे हिन्दुत्व कहती हैं। बड़े ही लगाव से वे लिखती हैं— “After a study of some 40 years and more of the great religions of the world, I find none so perfect, none so scientific, none so philosophic, and none so spiritual, as the great religion known by the name of Hinduism. Make no mistake; without Hinduism, India has no future. Hinduism is the soil into which India’s roots are struck, and torn out of that, she will inevitably wither, as a tree torn out from its place. And if Hindus do not maintain Hinduism, who shall save it? If India’s own children do not cling to her faith, who shall guard it? India alone can save India, and India and Hinduism are one.”
बेसेंट का हिन्दुत्व एक गहन बोध का हिन्दुत्व है। वे भारतीय स्मृति से इसकी प्रगतिशील चेतना को ग्रहण करती हैं। ईसाइयत के घोड़े पर सवार पश्चिमी साम्राज्यवाद के सामने वे इसकी मानवीयता को सामने रखती हैं और तथाकथित पश्चिमी डिमोक्रेसी, स्वतंत्रता,समानता के थोथे सिद्धातों की धज्जियाँ उडाती हैं। वे पश्चिम के इन तथाकथित उदारवादी दर्शनों के बरक्श सनातन भारतीय राजनैतिक संस्थाओं की महत्ता को उजागर करती हैं—“The argument that Democracy is foreign to India cannot be alleged by any well informed person. Maine and other historians recognize the fact that Democratic Institutions are essentially Aryan, and spread from India to Europe with the immigration of Aryan peoples. Panchayats, the ‘village republics’ had been the most stable institution of India, and only vanished during the last century under the pressure of the East India Company’s domination.” (From the Presidential Address – Dr. Annie Besant. I.N.C. Session, 1917, Calcutta.)
और शायद यही सब कारण थे की जब उन्होंने भारत की मिटटी पर अपना पहला कदम रखा तो सगर्व घोषणा की कि भारत में मेरा दूसरा जन्म हुआ है।
और ताज्जुब कि पंडित जवाहरलाल नेहरु जैसी धर्मनिरपेक्ष शख्सियत ने उनकी इसी आस्था पर यह ऐतिहासिक टिप्पणी की है और इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है—”आध्यात्मिक और राष्ट्रीय रूप से, भारतीय मध्य वर्ग पर एनी बेसेंट के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा।”
वैसे, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एनी बेसेंट के जीवन का सबसे महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था— विश्व गुरु का स्वप्न। वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में यह आज भी एक महनीय पर अधूरा प्रोजेक्ट है। भारत की प्राचीन पद्धति का सर्वांग अध्ययन कर उन्होंने इसे आकार दिया था। और इसके लिए उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को पहला ‘वाहन’ बनाया। थियोसाफिकल समाज ने जहाँ इस प्रोजेक्ट को खूब प्रचारित किया तो वहीं इस कारण उसमें अंतर्विरोध भी बने। बेसेंट ने स्वयं को कृष्णमूर्ति का संरक्षक बनाया और उन्हें दीक्षा दी। वे बेसेंट के भविष्य के स्वप्न थे जिन्हें वे ‘आर्डर आफ दी स्टार इन दी ईस्ट’ कहती थीं। आप ध्यान दें तो यह वही प्रोजेक्ट है जिसकी वकालत आजकल भाजपा और संघ करते हैं।
पर दु:खद है कि यह प्रोजेक्ट अधूरा रहा। 1929 में जिद्दू ने इस मिशन से स्वयं को अलग कर लिया, थियोसाफिकल सोसाइटी भी छोड़ दी और एक स्वतंत्र चेत्ता के रूप में विश्व को आपसी समन्वय और समानता का ज्ञान देने निकल पड़े। आश्चर्य है कि यह स्वतंत्र चेतना भी जिद्दू के भीतर स्वयं बेसेंट ने डाली थी। लेकिन इसके बावजूद भी बेसेंट जिद्दू से नाराज नहीं हुयीं। एनी बेसेंट की मृत्यु के बाद जब कृष्णमूर्ति से उनके संबंधों के बारे में पूछा गया तो जवाब में उन्होंने बेसेंट को लेकर एक अद्भुत बात कही है— “वह हमारी मां थीं, उन्होंने हमारी रक्षा की, पर उन्होंने यह कभी न कहा कि ‘यह करो’ या ‘यह न करो।’ कृष्णमूर्ति का यह कथन बेसेंट के चरित्र की लोकतांत्रिकता और विशालता को दर्शाता है।
खैर, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वे एक आदर्श प्रकार की शिक्षा का प्रसार पूरे विश्व में करना चाहती थीं। मैं उस शिक्षा-पद्धति पर ज्यादे नहीं बोलना चाहता। शिक्षा को लेकर बेसेंट के वे विचार बहुत व्यापक और सर्वविदित हैं तथा आप सब भी कम—बेसी जानते ही हैं। पर इस प्रसंग में मुझे बस एक दृश्य बरबस याद आता है। इसके माध्यम से ही शायद आप जान सकें की शिक्षा को लेकर उनकी उदात्तता का कितना महनीय स्तर था!
दृश्य बनारस का है। उन्होंने अपने सामने बैठे किशोरों को संबोधित करते हुए पूछा कि शिक्षा की क्या सार्थकता वे समझते हैं। छात्रों की ओर से प्रायः आदर्शवादी जवाब आए। अंत में जब लड़कों ने उन्ही से इसका जवाब माँगा तो अत्यंत लगाव से कहा उन्होंने— “तुम्हारी शिक्षा की सार्थकता तभी है जब तुम रोज समय मिलने पर, अपने जैसे किसी गरीब बच्चे को, स्वयं को मिला ज्ञान, बिना बदले में उनसे कुछ पाए, बाँट सको।” आश्चर्य है कि बेसेंट उस जमाने में ऐसा सोच रही थीं। जबकि आज भी पाठ्यक्रमों के को-क्युरीक्युलर, एक्स्ट्रा-क्युरीक्युलर एक्टिविटीज में यह पहल शामिल नहीं है। पर यह कितनी महत्त्वपूर्ण है, यह हम सब नकार नहीं सकते।
तो, भारत के प्रति यही मानस था उनका जो उन्हें हिंदी की तरफ धकेल रहा था। वे हिंदी में देश की पुनर्रचना और एकता का स्वप्न देख रही थीं। इसी उद्देश्य से सन् 1928 में उन्होंने मद्रास (चेन्नई) में हुए हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में हिन्दी-संदर्भ में एक प्रेरक वक्तव्य दिया था— “मेरा विश्वास है कि हिन्दी भारतवर्ष की मुख्य (संपर्क) भाषा होगी। मेरा विचार है कि भारतवर्ष की शिक्षा में हिन्दी अनिवार्य होनी चाहिए।”
जाहिर है कि उनके इस प्रकार के विचारों और गतिविधियों से हिन्दी-प्रसार को बाद में एक अनुकूल दिशा मिली। मातृभाषा की केन्द्रीयता के आधार पर एक ऐसे ही विश्व गुरु भारत की स्वप्नद्रष्टा थीं एनी बेसेंट।