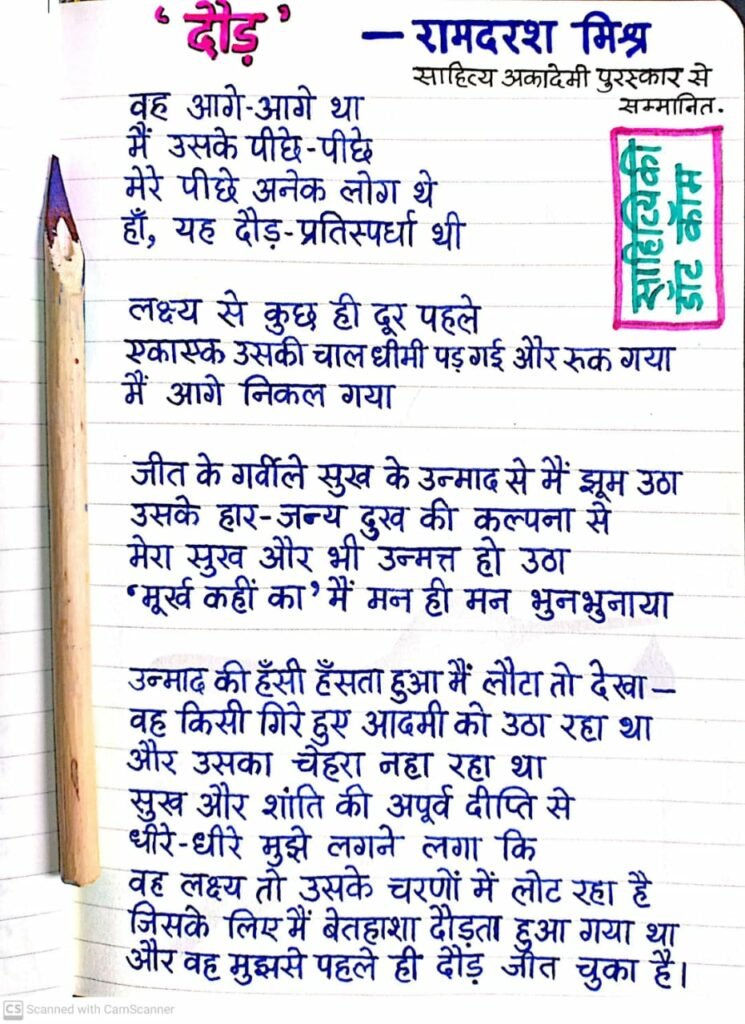हिंदी के वरिष्ठ कवि–आलोचक, कलाविद् एवं संस्कृतिकर्मी श्री अशोक वाजपेयी इस वर्ष 16 जनवरी को 80 वर्ष के हो गए। उनका जन्म 1941 में दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हुआ था। साहित्यिक लेखन की दुनिया में वे गत छह दशक से सक्रिय हैं और समसामयिक मुद्दों पर मुखर भी रहते हैं। लेखक–विचारक के रूप में उनकी ख्याति सुविदित है।
श्री अशोक वाजपेयी का लंबा काव्य–जीवन 16 कविता–संग्रहों और हिंदी आलोचना की 7 पुस्तकों में प्रतिफलित हुआ है। घर–परिवार, पूर्वज, प्रेम, प्रकृति, कलाएं, समकालीन सामाजिक परिदृश्य आदि उनकी कविता में चरितार्थ होते रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादेमी पुरस्कार, कबीर सम्मान, फ्रांस और पोलैंड के उच्च नागरिक सम्मान आदि मिले हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत, सैयद हैदर रज़ा आदि पर अंग्रेज़ी में आलोचना पुस्तकें लिखी हैं। वे भारत भवन के संस्थापक, सचिव और अध्यक्ष, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति तथा केंद्रीय ललित कला अकादेमी के अध्यक्ष रहे हैं। इन दिनों रज़ा फ़ाउण्डेशन के प्रबंध न्यासी हैं।
गत 11 जनवरी को श्री अशोक वाजपेयी से ‘साहित्यिकी डॉट कॉम‘ के संचालक संजीव सिन्हा ने उनकी साहित्यिक सक्रियता, हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा विचारधारा पर लम्बी बातचीत की। इस बातचीत को हम दो भागों में प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है पहला भाग (दूसरा भाग)—
? अशोकजी, आप इस वर्ष 16 जनवरी को अस्सी वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। आपने सक्रियतापूर्ण जीवन जिया है। अपने जीवन के इन अस्सी वर्षों को आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, जीवन तो हरेक का विविध होता है। यानी उसको किसी एक ढंग से देखने, महसूस करने या समझने का तरीका नहीं होता। हरेक के जीवन में विविधता होती है। सो, मेरे जीवन में भी रही है। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बहुत जल्दी बना लिया था कि मुझे साहित्यकार बनना है। मूलत: कवि बनना है तो अब कविता लिखते भी पैंसठ वर्ष पूरे हो जाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा ही हो जाएंगे। कविता बहुत जल्दी लिखना शुरू कर दी थी। कविता के बारे में जो मैंने दुनिया भर के दावे किए हैं, कई सूक्तियां कही हैं, कई स्थापनाएं गढ़ी हैं, उनका एक संचयन भी प्रकाशित हो रहा है।
मैंने यह भी अपने मन में तभी संकल्प बना लिया था कि मेरा काम सिर्फ कविता लिखना भर नहीं है बल्कि अपने समय–समाज में कविता की संभावना और जगह को बढ़ाना भी है, तो वो भी कोशिश करता रहा। आलोचना के माध्यम से भी कोशिश की। आयोजनों के माध्यम से भी। पत्रिकाएं मैंने बहुत निकाली। अब यह सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है कि पत्रिका मैंने छात्र–जीवन से निकालना शुरू कर दिया था। अब तक दस–बारह पत्रिकाएं हैं जो मैंने निकाली हैं समय–समय पर।
मेरे एक अध्यापक थे लक्ष्मीधर आचार्य, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा परिवार प्रशासकों का है इसलिए तुमको भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए, लेकिन मरना कवि की तरह। पैंतीस बरस रहा सिविल सेवा में और सिविल सेवा में कोई विशेष आकांक्षा नहीं रही सिवाय इसके कि मैं हाशिए पर रहा, और संस्कृति का क्षेत्र ऐसा है जो हमारी राजनीति–प्रशासन दोनों में हाशिए का है, सो उसमें कुछ करने की छूट भी मिली। सौभाग्य से संयोग भी ऐसे जुड़ते गए तो कुछ किया।
मेरे पिता के अनेक कटु अनुभव थे। उनके साथ बहुत विश्वासघात हुआ था, लेकिन वो मदद करने से कभी चूकते नहीं थे तो कुछ यह मेरे स्वभाव में भी आ गया कि अगर कोई मुझसे मदद मांगे या उसकी जरूरत मुझे लगेगी तो मुझे देने में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। तो वो भी कोशिश करता रहा। जहां जितने साधन जैसे बनते गए।
शुरू तो कविता से हुआ था लेकिन धीरे–धीरे कलाओं में दिलचस्पी जागी। जब मैं अपने पहले चरण में पांच वर्ष दिल्ली में था, सेंट स्टीफन कॉलेज में छात्र की तरह और बाद में अध्यापक की तरह, तो यहां जो तमाम गतिविधियां होती थीं, उनमें मैं जाने की कोशिश करता था। उससे एक संस्कार बनना शुरू हुआ। मेरी कलाओं में बहुत रूचि हो गई, विशेषकर शास्त्रीय संगीत, चित्रकला, नृत्य में। फिर इनके लिए कुछ करने का संयोग भी मिला। संस्थाएं भी मैंने बहुत बनाई, तो ये सब करता रहा। लेकिन बहुत सारे काम हैं जो नहीं कर पाया, तो मेरी सफलताओं की गाथा जितनी लंबी है, उससे कई गुना लंबी है विफलताओं की गाथा।
? आप साहित्य की तरफ कैसे आकृष्ट हुए थे?
मैं अपने माता–पिता की पहली संतान था। हमलोग आठ भाई–बहन हैं, चार भाई और चार बहन। मैं सबसे बड़ा हूं और मेरा जो सबसे छोटा भाई है उदयन, वह भी साहित्य में है। जैसे मैं प्रशासन में रहकर साहित्य में रहा, वैसे वो मेडिकल कॉलेज में अध्यापक होने के बावजूद साहित्य में। तो घर में एक पढ़ा–लिखा शिक्षित वर्ग था। हमारे बाबा किसान थे लेकिन हमारे पिता ने बनारस और इलाहाबाद से बीए–एमए वगैरह पढ़ा था। हमारे एक ताऊ थे जिनकी बड़ी जल्दी मृत्यु हो गई। मैं तब बहुत छोटा था। वे प्रसाद, निराला, नंद दुलारे वाजपेयी; इन सबके मित्र थे। तो कुछ हल्का सा इस तरह का वातावरण था लेकिन साहित्य में जाने का कोई बहुत उत्साह देनेवाला घर में वातावरण नहीं था। पढ़ा–लिखा परिवार था, सब एमए–पीएचडी वगैरह करते रहे। सभी भाई–बहनों ने किया। लेकिन सबसे बड़ा लड़का जो होता है वो थोड़ा अकेला भी होता है न, उससे सबकी दूरी होती है, उस समय शायद मैंने शब्दों से खेलना शुरू किया होगा और फिर धीरे–धीरे लगा कि शब्द से कुछ हो सकता है।
? प्रारंभ में किन लेखकों का आप पर प्रभाव रहा था?
उस समय हम पर जो प्रभाव पड़े थे, वो तीन–चार किस्म के थे। एक तो चूंकि हम मध्यप्रदेश में थे और मध्यप्रदेश के ही एक कवि उन दिनों लोकप्रिय हो रहे थे–भवानी प्रसाद मिश्र, तो थोड़ा आरंभिक प्रभाव उनका पड़ा। फिर जब अज्ञेय को पढ़ा तो उनका भी प्रभाव हुआ। शमशेर बहादुर सिंह की जो अल्प–वागर्थता थी, उसकी ओर भी आकर्षित हुआ। मुक्तिबोध से जब संपर्क हुआ तब वो, मैं सागर विश्वविद्यालय में छात्र था, वहां आते थे, तो आरंभिक प्रभाव इन तीन–चार साहित्यकारों का था। फिर बाद में रघुवीर सहाय से भी कुछ सीखने को मिला। मुझे यह कहना चाहिए कि उस समय वातावरण ऐसा था कि यद्यपि मैं अज्ञातकुलशील ही था, लेकिन मुझे कल्पना, वसुधा, युगचेतना, ज्ञानोदय, इन सबमें बहुत आसानी से कविताएं प्रकाशित करने का अवसर मिलता रहा।
? क्या आपने आरंभ में ही विदेशी लेखकों को पढ़ना शुरू कर दिया था, उन सबका किस तरह का प्रभाव पड़ा था?
मैं जब विश्वविद्यालय में गया तो एक साल विज्ञान का विद्यार्थी था। उसमें मैंने विश्वविद्यालय में टॉप भी किया, फिर छोड़ दिया कि साहित्य वगैरह पढ़ेंगे। उस समय रिल्के, काफ्का, पाब्लो नेरूदा; इन सब लेखकों की किताबें सौभाग्य से सागर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में थीं। तब एक व्हीटलोन एग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका से गेहूं आयात किया गया था तो उसके अंतर्गत अमेरिकी प्रकाशकों की बहुत सारी पुस्तकें भेंट में आई थीं। उन पुस्तकों में बहुत सारी इस तरह की पुस्तकें थीं कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आया तो यहां वे पुस्तकें नहीं थीं जो सागर विश्वविद्यालय में थीं। काफ्का, अल्बेयर कामू की पुस्तकें थीं, ‘पार्टीजन रिव्यू’ पत्रिका आती थी। फिर एक वर्ष नामवर सिंह यहां अध्यापक थे। यद्यपि वो हिंदी के अध्यापक थे। मैं हिंदी का छात्र नहीं था। मैं इतिहास, संस्कृत और अंग्रेजी का छात्र था, पर उनसे मेरी अच्छी मित्रता सी हो गई। उनके माध्यम से भी कुछ लेखकों का पता चला, किर्के गार्ड आदि के बारे में।
जब मैं दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज आया तो मुझे बहुत ही अटपटा लगा क्योंकि सुबह से शाम तक अंग्रेजी बोलने की मुझे आदत ही नहीं थी। अपनी भाषा सुनने का अवसर ही बहुत कम था। बाद में तो मैं अकसर भाग जाया करता था कनॉट प्लेस, जहां श्रीकांत वर्मा, कमलेश, सुरेंद्र भल्ला, बाद में प्रयाग शुक्ल आ गए थे, अशोक सेकसरिया, हमारी मंडली चलती थी, ये सब लोग होते थे।
मैंने अठारह बरस की उम्र में, एक डच कवि थे ह्यूगोक्लॉस, उनकी कविता का अनुवाद किया था। ये कहीं छपी थीं। ह्यूगोक्लॉस बहुत बड़े लेखक और उपन्यासकार बने।
? हमारी पांच हजार वर्षों की संस्कृति है, इसकी उज्ज्वल जीवंत परंपरा है, और इससे विशिष्ट जीवन–दृष्टि भी मिलती है। पाश्चात्य लेखक तो इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं लेकिन हिंदी साहित्य के लेखक भारतीय संस्कृति से दूरी बररते हैं, ऐसा क्यों?
नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग हैं, शायद दूरी बरतते हैं। जिसको आप आम तौर पर वामपंथी समुदाय कहते हैं, उसमें एक समुदाय ऐसा दुर्भाग्य से रहा है जिसको भारतीय परंपरा की सब पतनशीलता पूरी तरह नजर आती है। हर परंपरा में पतनशीलता है। पश्चिम की परंपराओं में भी ऐसे तत्त्व मिल जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा समझदार, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा जिज्ञासु साहित्यकार हैं उस वामपंथ में भी, जैसे रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, इतिहासकारों में रोमिला थापर वगैरह, उनमें यह समस्या नहीं रही है।
भारत में एक बड़ी भारी समस्या यह है कि यहां परंपरा में इतिहास तो शामिल है लेकिन इतिहास में परंपरा समा नहीं पाती है और हम इतने इतिहासबद्ध समाज संभवत: नहीं हैं, जितने कि हम परंपराजीवी समाज हैं। परंपरा में बहुत सारी चीजें हैं, जिनको हमने व्यर्थ ही गंवा दिया है। आधुनिकता की जो झोंक आई भारत में, पश्चिम प्रेरित आधुनिकता, उसमें जो स्वयं हमारी आधुनिकता थी, तब भी करीब चार सौ–पांच सौ बरस पुरानी हो चुकी थी। अगर हम उसको सरहपा और कबीर से शुरू माने।
? आधुनिक शब्द को लेकर आपने एक बार कहा था कि मिथिला के विद्वान् उदयनाचार्य ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया था।
आधुनिक शब्द–प्रयोग के बारे में हमारे मित्र मुकुंद लाठ ने बताया था। मुझे पता नहीं था कि दरभंगा में एक नव्यनैयायिक हुए उदयनाचार्य। उन्होंने अपने को कश्मीर शैव न्याय से अलग करते हुए यह कहा, ‘ते प्राचीना: वयं आधुनिका:।’ कि वो लोग तो प्राचीन हैं, हम आधुनिक हैं। यद्यपि वो उसी न्याय परंपरा में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे।
अकसर पश्चिम में परंपरा और परिवर्तन के बीच एक तनाव और विरोध माना जाता है और अकसर परंपरा से बाहर परिवर्तन होता है। हमारे यहां जितने परिवर्तन हुए हैं, मूलगामी और दूरगामी परिवर्तन, वो परंपरा के अंतर्गत ही हुए हैं, तभी परंपरा इतने वर्षों तक जीवित रही है। कई बार मुझे लगता है कि जो भी जड़–तत्त्व हमारे यहां हैं, वो सारे जड़–तत्त्व अब धर्मों में हैं। क्योंकि धर्म तो बदलते नहीं हैं। अगर दो हजार साल पहले ही सारा विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या हम एक मरणोत्तर जीवन दो हजार साल से जी रहे हैं? हर चीज अगर परिवर्तित हुई है तो धर्म परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? हो रहे थे, हुए लेकिन अब जाकर जड़ हो गए हैं और इसलिए इस समय मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो भारतीय धर्म है, भारत में जो भी धर्म हैं, वे सभी परंपरा से अलग पड़ गए। वे अब अपनी ही परंपरा में नहीं हैं। सारे धर्म इस समय अनुष्ठानों में बदल दिए गए है।
मैं हिंदू हूं, यद्यपि मैं नास्तिक हूं। मुझे आस्था का वरदान नहीं मिला है, लेकिन मैं हिंदू हो सकता हूं। मैं किसी मंदिर में विश्वास करूं या किसी देवता में विश्वास करूं, मेरा धर्म इसकी बाध्यता नहीं करता। इसलिए अभी जो हिंदुत्व है, उसका हिंदू धर्म से कुछ लेना–देना नहीं है। वो तो हिंदू धर्म को एक राजनीतिक संरचना में बदलकर उसका शोषण करने की विचारधारा है। ये ‘विचारधारा’ है।
? ईश्वर के संबंध में आपके क्या विचार है?
मनुष्य के जो सबसे क्रांतिकारी और दूरगामी आविष्कार हैं, उनमें तीन हैं। एक है–भाषा। मैं यह कहता रहा हूं, पृथ्वी, पृथ्वी ही बनी रहती अगर भाषा न होती। पृथ्वी को संसार में बदलने का काम भाषा ने किया। हमारे पास भाषा है इसलिए पृथ्वी सिर्फ पृथ्वी नहीं है, संसार भी है।
दूसरा है–अमूर्तन। मतलब भाषा भी एक तरह से अमूर्तन ही है। मेज शब्द का मेज नाम की वस्तु से क्या संबंध है, कुछ नहीं है। हमने उसको मेज कह दिया, अगर पहले कभी कुर्सी कह दिया होता तो कुर्सी हो जाती। अमूर्तन ने बहुत सारा ज्ञान–विज्ञान पैदा किया। गणित उससे पैदा हुआ, संगीत पैदा हुआ।
और तीसरा है–अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है कि हम सिर्फ पृथ्वी पर नहीं रहते, ब्रह्मांड में रहते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम एक बड़ी ज्यादा ब्रह्मांडव्यापी सचाई का हिस्सा हैं, और उसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हैं और हर चीज एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। इसी में एक विधाता की कल्पना की, क्योंकि ईश्वर अपने आप में और धर्म भी अपने आप में महान् आविष्कार है।
मुझे धार्मिक होने का शौक नहीं है, हालांकि वो अलग बात है, लेकिन धर्म ने संसार भर के इतिहास में महान् साहित्य, महान् कला और महान् चिंतकों को जन्म दिया है। मुझे यह हक नहीं है कि मैं किसी दूसरे को विवश करूं कि चूंकि मैं विश्वास नहीं करता इसलिए मैं दूसरे से बेहतर हूं। तो ईश्वर एक आविष्कार है, क्योंकि क्या गिलहरियों और कुत्तों का ईश्वर होता है? क्या पक्षियों–चीटियों और पर्वतों–नदियों का ईश्वर होता है? क्या उनमें ईश्वर की अवधारणा है? तो ईश्वर बहुत ही मानवीय अवधारणा है।
? आप अपने को आध्यात्मिक व्यक्ति तो कहते हैं लेकिन धार्मिक नहीं, क्या अंतर है धार्मिकता और आध्यात्मिकता में?
धर्म की पद्धतियां, उसके रीति–रिवाज, उसके अनुष्ठान, उन सबका पालन करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना; ये सब धार्मिकता के अंग हैं, इन सबमें मेरी कोई गति नहीं है। मेरा अध्यात्म इस ब्रह्मांडव्यापी सचाई में अपनी भागीदारी और अपनी मौजूदगी का एहतराम है। संसार में हम ब्रह्मांड के हिस्से हैं, और हर चीज एक–दूसरे से जुड़ी हैं, ये अध्यात्म है। मैं ये भी कहता रहा हूं कि इसकी नदियां, पर्वत, जंगल, पेड़–पौधे, प्रकृति और जो दूसरा प्राणी जगत है, वो तो मनुष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है लेकिन मनुष्य उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक कर रहा है, कोताही कर रहा है। यह एक स्तर पर मेरे लिए आध्यात्मिक प्रश्न है। यह एक आध्यात्मिक तनाव है कि दूसरे तो आपके प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाएं, आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूकें।
? हिंदी ज्ञान की भाषा बने, इसमें मौलिक विचार प्रस्तुत हों, इसको लेकर आप वासुदेव शरण अग्रवाल, भगतवत शरण उपाध्याय, रायकृष्ण दास आदि के योगदान का उल्लेख करते रहे हैं। क्या अभी इस तरह का लेखन करनेवाले हिंदी में हैं?
आखिर ज्ञान कहां होगा? या तो विश्वविद्यालयों में होगा, शिक्षा के क्षेत्र में होगा या अध्यात्म के क्षेत्र में होगा। पिछले सत्तर बरस जो मैं जानता हूं, उसमें ये आरंभिक छोड़ दें जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवतशरण उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काशी प्रसाद जायसवाल, रायकृष्ण दास, राहुल सांकृत्यायन इत्यादि लोग थे जिन्होंने ज्ञान के कुछ अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्रों में ही काम किया, इतिहास, पुरातत्त्व, परंपरा इत्यादि में, पर ज्ञान–विज्ञान के और सारे जो क्षेत्र हैं, इसमें हमने कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं पैदा किया, कोई बड़ा मनोवैज्ञानिक नहीं पैदा किया।
लेकिन इधर, अभय कुमार दुबे एक पत्रिका निकालते हैं ‘प्रतिमान’, उसमें मूल हिंदी में बहुत सारा, खासकर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अब कुछ अच्छा काम हो रहा है, वो एक आशा बनाता है, इसलिए मैं उस पत्रिका का बड़ा प्रशंसक हूं। अभी उन्होंने कोरोना पर एक अंक निकाला है, जिसमें बहुत ही बढि़या सामग्री है। ऐसी सामग्री शायद किसी अंग्रेजी पत्रिका ने नहीं निकाली।
हमारे यहां मुकुंद लाठ थे, उन्होंने इस पर बहुत विचार किया था, लेकिन उनको हिंदी साहित्य में कोई जगह मिली नहीं। वे दर्शन के क्षेत्र में मान लिए गए, जबकि उन्होंने संगीत, नृत्य, नाटक और साहित्य पर भी बहुत अच्छा लिखा है। यशदेव शल्य हैं राजस्थान में। दयाकृष्ण थे, जिन्होंने हिंदी में काम किया था, तो ऐसे लोग रहे हैं।
अब युवा लोग हैं, उनमें प्रमोद रंजन हैं, जिन्होंने कोरोना पर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लेख लिखा है। सदन झा हैं, जिन्होंने संभवत: इस तरह का काम किया है। तो ऐसे लोग कम हैं, ये हिंदी की मुख्यधारा में नहीं माने जाते।
? हिंदी अंचल में सुधार आंदोलन की धारा कमजोर है। इस अंचल के सामाजिक–साहित्यिक उत्थान के लिए क्या किए जाने चाहिए?
दो–तीन बातें हैं। एक यह है कि सामाजिक सुधार का आंदोलन बहुत कम हुआ हिंदी अंचल में। इसलिए हिंदी अंचल सबसे मंदगति मंदमति, धर्मांध, सांप्रदायिक, जातिवादी, इसी में फंसा हुआ है। समाज सुधार जितना महाराष्ट्र में हुआ, एक जमाने में गुजरात में हुआ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में हुआ, बंगाल में भी हुआ, वो हमारे यहां हुआ नहीं। आखिर इतना बड़ा अंचल है, इसमें आज भी वही जातिप्रथा चली हुई है, आज भी दलित अगर घोड़े पर चढ़कर अपनी शादी–बरात में जाए तो आप उसे गोली मार देंगे, ये क्या बात हुई?
इस समय हिंदी के लिए बड़ा भारी संकट है। और ये हिंदीभाषी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। उनकी भाषा लगातार धर्मांधता, सांप्रदायिकता, हिंसा, हत्या, बलात्कार की भाषा बन चुकी है, वो गालियों की भाषा बनी हुई है, वो झगड़ों की भाषा बनी हुई है, वो घृणा की भाषा बन रही है, और ये सब हिंदी भाषी समाज स्वयं कर रहा है। आखिर उसी ने ये सत्ताएं चुनी हैं, उसी ने ये सब लोग चुने हैं।
हिंदी साहित्य इस समय हिंदी समाज का असला राजनैतिक प्रतिपक्ष है। बाकी सब एक ही थैली के चट्टे–बट्टे हैं। इसलिए यह कोई विचारधारा का संघर्ष नहीं है।
दक्षिण में जब हिंदी को फिर से लादने की कोशिश की जा रही है, अगर विरोध होता है तो उसका सिर्फ ये पक्ष नहीं है कि हिंदी वालों को उससे कुछ बड़ा मिलनेवाला है। हिंदी भाषा इस समय इन चीजों का पर्याय बन रही है।
हिंदी अंचल में अभी भी महत्त्वपूर्ण लेखक चाहे वो युवा हों, अधेड़ हों या बूढ़े हो गए हों, उनमें से किसी को भी इन सबके समर्थन में नहीं रखा जा सकता, किसी ने पाला नहीं बदला। छह बरस हो गए सरकार को, लेकिन उसके पाले में कोई गया नहीं, जो पहले से ही उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, सो हैं, अभी भी रखते हैं, और उनमें जहां तक मेरी नजर है, कोई बहुत महत्त्वपूर्ण लेखक तो दिखाई नहीं देता।
? नरेन्द्र कोहली, चित्रा मुद्गल, कमल किशोर गोयनका….।
दो चार हैं ये। ये पहले से ही थे। इन्होंने पाला नहीं बदला। लेकिन जिनको आप हिंदी की एक महत्त्वपूर्ण परंपरा में रखेंगे, इनमें से एकाध ही कोई आएगा।
? आप कभी लेखक संगठन से भी नहीं जुड़े?
मैं किसी लेखक संगठन से नहीं जुड़ा। न मैंने संगठन बनाया, न किसी संगठन में शामिल हुआ। कभी–कभार ऐसा हुआ है कि लेखक संगठनों ने अपने आयोजनों में मुझे बुलाया है तो मैं साभार और सहर्ष गया हूं, और अपनी बात रखी है। पहले तो खैर बुलाते ही नहीं थे, हमारा बहिष्कार ही करते थे, लेकिन एक बार याद है कि मध्यप्रदेश में किसी लेखक संघ ने शायद बिलासपुर या कहीं और अधिवेशन था उनका, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया भारत भवन के बहिष्कार का। जिस दिन पारित हुआ उसके रात को हरिशंकर परसाई, जो उसके अध्यक्ष थे, का फोन आया कि कल तुम अखबारों में पढ़ोगे, उसको लेकर तुम चिंतित मत होना। तुम जो कर रहे हो, वो ठीक है। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसे लोग भी थे। और ऐसे लोग भी थे जो अवसरवादी थे। उनको मैंने अचूक अवसरवादी कहने में कभी कोई संकोच भी नहीं किया है।
ऐसा भी है कि सीधे–सीधे तो जिंदगी चलती नहीं है, उसके इधर–उधर दुनिया भर के मोड़ आते हैं, कुछ प्रभाव आते हैं, कुछ दबाव आते हैं, तो उनसे निपटकर अपने इस सामाजिक अंत:करण को जीवित रखना और सजग रहना, यह कोशिश करता रहा। कितना हो पाया, ये तो दूसरे जानेंगे।
? तो साहित्यकारों का संगठन आपको जरूरी लगता है या नहीं?
साहित्यकारों का संगठन जरूरी लगता है, दो कारणों से। एक कि वो अगर बहुलतावादी हो। उसमें अगर चित्रा मुद्गल, नरेन्द्र कोहली को भी जगह मिले। दो भी रहे तो उनको खारिज करके नहीं हो, उनको शामिल करके हो और खुला मंच हो, जिसमें साहित्य की समस्याओं पर बातचीत हो, दूसरे जो व्यावसायिक मसले हैं लेखकों के, यानी रॉयल्टी, प्रकाशन की सुविधाएं और उनके मेडिकल, खर्च वगैरह की व्यवस्था, पेंशन…इन सबका भी विचार करके हो। हमने कोशिश की थी। संगठन का काम इस दिशा में ज्यादा होना चाहिए। अभी तो अलग विचार मंच बने हुए हैं।
पीइएन जैसा संगठन हो। लेखकों की स्वतंत्रता पर जहां–जहां हमला होता है, अगर किसी लेखक को परेशान किया जा रहा है, उसको बेवजह जेल में डाल दिया जाता है, जब अभिव्यक्ति की आजादी पर कटौती हो रही हो तो उस समय लेखकों को अपनी आवाज उठानी चाहिए।
? आपकी राजनीति क्या है?
हमारी राजनीति बहुलता की राजनीति है। स्वतंत्रता, समता और न्याय के मूल्यों में किसी मूल्य को दूसरे मूल्य से कमतर न मानने की राजनीति है। हमारी राजनीति यह है कि जैसे और अनुशासन हैं, जिनको ज्ञान पर हक है, ठीक उसी तरह से साहित्य और कलाओं को भी ज्ञान पर हक है। वो भी ज्ञान की विधाएं हैं। ये राजनीति है।
? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, ललित कला और रंगमंच आदि के प्रति आपकी दिलचस्पी कैसे हुई?
दिल्ली आने से पहले थोड़ी–थोड़ी दिलचस्पी सागर में जाग गई थी। मुझे लगता था कि बहुत छोटे शहर में हूं और संसार तो बहुत बड़ा है। मेरा जो पहला कविता–संग्रह है उसमें अली अकबर खां के सरोद वादन पर एक कविता है, मकबूल फिदा हुसेन के एक चित्र पर भी एक कविता है, शमशेर बहादुर सिंह के पहले कविता–संग्रह पर एक कविता है और खजुराहो पर भी एक कविता है, तो एक तरह की सर्जनात्मकता का स्फुरण सा हो रहा था, जो कि दिल्ली में आकर एक गहरे संस्कार में बदल गया। यहां बहुत सारे लोग थे। नाटक होते थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नाटक होते थे। अलकाजी थे। हबीब तनवीर थे। बड़े–बड़े संगीतकारों को मैंने पहली बार यहीं सुना। चित्रकला में दिलचस्पी रामकुमार, हुसेन, सतीश गुजराल और धनराज भगत की प्रदर्शनियों से हुई।
मुझे लगता यह रहा कि अंतत: कविता सिर्फ कविता में नहीं होती, जैसे कविता कभी–कभी गद्य में भी होती है। क्योंकि एक लय बनाती है। वैसे ही कविता दूसरी कलाओं में भी है। वो दूसरा रूप लेती है। उसके नियम और उसकी परिपाटियां अलग होंगी, उसकी स्मृतियां अलग होंगी, लेकिन वो एक तरह से कविता है। दूसरी तरफ यह कि जो कविता का सच है, उससे रंगमंच का सच अलग है, उससे संगीत का सच अलग है, चूंकि मैं सचों की बहुलता में विश्वास करनेवाला व्यक्ति हूं, मुझे लगा कि ये अलग–अलग सच है, इनको जानना भी चाहिए, इनका एहतराम भी करना चाहिए।
? आपने एक कवित्रयी बनाई है–अज्ञेय, शमशेर और मुक्तिबोध की। आप इन तीनों कवियों को महत्त्वपूर्ण क्यों मानते हैं?
मैंने तो एक पूरी किताब ही लिखी है–‘कविता के तीन दरवाजे।’ मैंने उसमें कहा था कि अज्ञेय विवेक के कवि हैं। मुक्तिबोध अतिरेक के कवि हैं और शमशेर विवेक और अतिरेक के बीच नाजुक रूप से संतुलित हैं। अज्ञेय की कविता में बहुत ही सुगठित विन्यास है, शमशेर में सौंदर्य की अपार रंगभूमि है और मुक्तिबोध में खुरदरा यथार्थ और बीहड़ स्थापत्य है। तो अपने समय की सचाई को जानने के लिए ये तीनों मुझे जरूरी लगते हैं।
अज्ञेय की एक विशेषता इन दोनों के मुकाबले यह भी है कि अज्ञेय ने कविता की संभावना को अपने समय में बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। चार सप्तक तो निकाले ही, पत्रिकाएं निकालीं, प्रतीक निकाला, नया प्रतीक निकाला। चौथा सप्तक आते–आते उनकी पकड़ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। महत्त्वपूर्ण तो तीन सप्तक हैं। यानी तीन सप्तकों में जो इक्कीस कवि हैं, उनमें से कम से कम पंद्रह कवि महत्त्वपूर्ण निकले। यह बड़ी बात है।
मैं संकोच से कहता हूं, फिर मैंने ‘पहचान’ में पंद्रह युवा कवियों के पहले कविता–संग्रह छापे, जिनमें विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, हितेन्द्र कुमार, कमलेश, ज्ञानेन्द्रपति, चंद्रकांत देवताले, सौमित्र मोहन–ये सब शामिल थे। इनके पहले कविता–संग्रह हमने छापे थे। वो एक तरह से अज्ञेय की ही प्रेरणा थी।
शमशेर हिंदी में सबसे अधिक उर्दू कवि हैं। हिंदी गद्य में सबसे अधिक उर्दू गद्यकार कृष्ण बलदेव वैद हैं। उन्होंने उर्दू का रचाव पूरा हिंदी में रखा है।
देखिए, हमारी हिंदी को। संस्कृत, अपभ्रंश, फिर उर्दू यानी अरबी–फारसी–उर्दू और बाद में अंग्रेजी, इन चारों से बनी हिंदी। हमारे मित्र थे विद्यानिवास मिश्र। वे एक वाक्य बताते थे–‘‘मैं कमरे में घुसा, कमीज उतारकर कुर्सी पर डाल दी, खिड़की खोली, आकाश की तरफ देखा, टेलीविजन चला दिया, इसमें पांच भाषाएं हैं। कमरा इतालवी से, कमीज अरबी से, कुर्सी पुर्तगीज से, आकाश संस्कृत से, टेलीविजन अंग्रेजी से और बाकी हिंदी।
मुक्तिबोध ने एक क्लासिक लिखा ‘अंधेरे में’। लिखा तो 1963–64 में और वो सच हुआ अब जाकर। उसमें जो दृश्यावली है, वो आज की दृश्यावली नजर आती है, हिंसा, अंधकार आदि।
बड़ा कवि दो काम कर सकता है। पहला, आपको अपने अंधेरे को पहचानने में, उसकी शिनाख्त करने में मदद करें और दूसरा, आपको रोशनी दिखाए। हो सकता है कोई इतना बड़ा कवि हो, जो दोनों काम एक साथ कर दे, जैसे–तुलसीदास। जैसे कबीर, अंधेरा भी दिखाते हैं, उजाला भी दिखाते हैं। ये अलग–अलग हो सकता है।
हिंदी आलोचना में बहुत मुश्किल हुई है, खासकर हमारे विश्वविद्यालयों में जो अकादमिक दिनचर्या है उसमें हिंदी के पूरे वैभव को, उसकी पूरी विविधता को ठीक से प्रगट नहीं होने दिया। उसको व्यर्थ की संस्कृतनिष्ठ बना देते हैं। हमारे यहां तत्सम और तद्भव दो रूप थे। हमने बहुत सारे शब्दों को तत्सम स्वीकार नहीं किया, तद्भव स्वीकार किया। जैसे, लैलटर्न–हमने लालटेन बना दिया। रेलगाड़ी–‘रेल’ वहां की ले ली, ‘गाड़ी’ अपनी लगा दी। ये भाषा की अपनी आविष्कारक क्षमता है और दूसरी तरफ उसकी ग्रहणशीलता है। हिंदी भारत की सबसे आतिथेय भाषा है। अगर इस समय आपको जानना हो कि मोटे तौर पर मूल्यवान या क्लासिक कृतियां भारतीय भाषाओं में कौन सी है, तो आपको उसका हिंदी में अनुवाद में मिल जाएगा। जितना अधिक अनुवाद हिंदी में होता है उतना मलयालम और शायद मराठी, इन दो भाषाओं में होता है। सबसे कम अनुवाद दूसरी भाषाओं से बांग्ला में होता है। बांग्ला सबसे अनाथितेय भाषा है। तो हिंदी को ये एक गौरव है।
हमको विश्वभाषा बनने का एक मूर्खतापूर्ण चस्का सताए रखता है। आप विश्वभाषा न हैं, न होंगे। विश्वभाषा पहले अपने देश में तो बने। हिंदीभाषी राज्य आज तक तय नहीं कर पाए कि कलेक्टर को, कमिश्नर को एक ही नाम दिया जाए। या कलेक्टर–कमिश्नर ही कहो, अगर सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है तो। स्टेशन को कुछ और तो आप नहीं कहते। टेलीफोन को आप कुछ और नहीं कहते। दूरभाष कौन कहता है! सब कहते हैं, फोन करेंगे। जुबान ने इसको मान लिया है। दूसरी तरफ, आपका खुद राजनयिक व्यवहार हिंदी में नहीं है। किस देश के साथ आप हिंदी में राजनयिक व्यवहार करते हैं? तो वह कहां से विश्वभाषा बन जाएगी? जिस भाषा में पर्याप्त ज्ञानमूलक साहित्य नहीं है, पर्याप्त विज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि नहीं है, उस भाषा को विश्वभाषा कैसे बना दिया जाएगा? कौन बना देगा? ये सब व्यर्थ के प्रलोभन हम अपने लिए बनाते हैं। हमारे यहां भाषा का दुष्प्रयोग सार्वजनिक रूप से हो रहा है।
? हिंदी के अखबार भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।
हिंदी के अखबार तो विचारणीय ही नहीं रह गए हैं। उनको तो पढ़ा भी नहीं जा सकता। इतनी खराब भाषा लिखते हैं। सीएम लिखने लगे आजकल। मराठी में पंतप्रधान कहते हैं उसको, पंतप्रधान की जगह वो कभी सीएम नहीं लिखेंगे। अपनी भाषा से लगाव भी हिंदी में बहुत कम है। सबसे कम है। यानी भारतीय भाषाओं में अपनी मातृभाषा से प्रेम करनेवाले लोग सबसे कम हिंदी में है, अनुपात की दृष्टि से।
हिंदी वालों की बड़ी मुश्किल ये है कि वे दूसरी भारतीय भाषाएं नहीं सीखते। अगर आपको राष्ट्रभाषा बनने का इतना शौक है, अव्वल तो इसकी क्या जरूरत है लेकिन अगर बनना था तो ऐसा होना सकना चाहिए था कि हिंदी के विश्वविद्यालयों में या हिंदी के विभागों में या विश्वविद्यालय के विभागों में कम से कम एक दो विशेषज्ञ आलोचक होते। मान लीजिए कन्नड़ उपन्यास के या बांग्ला कविता के या मलयालम उपन्यास के या असमिया के, जिन्होंने वो भाषा पढ़ी होती, उन्होंने अनुवाद किया होता। अभी क्या होता है कि उडि़याभाषी को हिंदी पढ़ना पड़ता है, कन्नड़भाषी हिंदी पढ़ता है और अपनी भाषा से अनुवाद हिंदी में करता है, वैसे ही उसकी हिंदी अटपटी सी रहती है। यदि श्रीनिवास राव ने अनुवाद किया है तो आप क्यों पढ़ेंगे, पता ही नहीं श्रीनिवास राव कौन है, लेकिन मान लीजिए वही अनुवाद इलाचन्द्र जोशी ने किया है तो आप पढ़ेंगे कि इलाचन्द्र जोशी ने किया है। तो ये हिंदी वालों ने अपने साथ ही बहुत विश्वासघात किया है।
? आप कुछ प्रमुख कवियों, कथाकारों, आलोचकों के नाम बताइए, जिन्हें आवश्यक रूप से पढ़ा जाना चाहिए।
सीधे हिंदी साहित्य पढ़ने लग जाएं और पहले को न पढ़ें तो यह उचित नहीं हैं। हमारे सबसे बड़े कवि तो भक्तकाल के ही हैं। कबीर, तुलसीदास, मीरा, सूरदास। उसके बाद के रीतिकाल के कवि भी बहुत अच्छे हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए, वो भी बड़े कवि हैं। देव, पद्माकर, बिहारी, केशवदास, जिनको ये सामंती–सामंती कहकर टाल रखा है, उनमें भी हिंदी का, खासकर अवधी और ब्रज का जो संगीत और जो छटा है, वो तो अद्भुत है।
फिर उसके बाद मैथिलीशरण गुप्त को पढ़ लें। मैथिलीशरण गुप्त एक जमाने में बड़े लोकप्रिय कवि थे। उसके बाद फिर छायावाद के कवि हैं, प्रसाद, निराला, पंत। प्रसाद को कम पढ़ा गया है। जबकि प्रसाद ने पूर्व–पश्चिम की चेतना के बीच में जो द्वैत है उसको बहुत तीखी नजर से परखा था। ‘कामायनी’ एक अद्भुत महाकाव्य है। ‘राम की शक्ति पूजा’ को पढ़ना चाहिए। किसी और को चाहे न पढ़ें, रामचंद्र शुक्ल को जरूर पढ़ना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने इतने अद्भुत कविता के उदाहरण दिए हैं। हमने इनका पूरा संकलन छापा था विश्वविद्यालय की ओर से। ‘कविता का शुक्ल पक्ष’ नाम से। बच्चन सिंह थे बनारस में, उन्होंने तैयार किया था हमारे लिए। विशेषत: महादेवी का गद्य बहुत पठनीय है। आज स्त्रीबोध इतना प्रबल है, उसकी खड़ी बोली में पहली आवाज तो महादेवी थीं।
उसके बाद फिर अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना–जिनको सब भूल ही गए, दुष्यंत कुमार, विजयदेव नारायण साही और उसके बाद धूमिल, कमलेश, विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, ज्ञानेन्द्रपति, मंगलेश डबराल, असद जैदी।
दिनकर–बच्चन को भी पढ़ना चाहिए। मैं उस कविता से बहुत प्रभावित नहीं हूं, लेकिन हिंदी की एक परंपरा तो थी ही वो। उसने भले बुद्धि को देशनिकाला दे दिया था कविता से, लेकिन बहरहाल, कविता को लोकप्रिय बनाया था, उसमें उनका योगदान है।
हमने त्रिमूर्ति जैसे कविता में बनाई, वैसे गद्य में बनाई–कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद। प्रेमचंद और जैनेन्द्र कुमार को पढ़ना चाहिए। जैनेन्द्र कुमार का चिंतन भी बहुत अच्छा है। फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ना चाहिए।
कहानी मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूं। मुझे लगता है कि कवियों ने जो कहानियां लिखी हैं उसका दुर्लक्ष्य किया गया है। मेरे हिसाब से रघुवीर सहाय, कुंवरनारायण, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, इन्होंने जो कहानियां लिखी है, उसे पढ़ना चाहिए। नरेश मेहता के उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए, खासकर ‘यह पथ बंधु था,’ यह बड़ा उपन्यास है। रांगेय राघव की एक कहानी है ‘गदल’, बहुत ही अद्भुत कहानी है। धर्मवीर भारती की कहानियां पढ़ना चाहिए–‘अंधा युग’ और ‘सूरज का सातवां घोड़ा’ और कुछ कहानियां, ‘बंद गली का आखिरी मकान’ बहुत अच्छी है।
अज्ञेय का शेखर एक जीवनी और उनका हर किस्म का गद्य पढ़ना चाहिए। अज्ञेय एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने जिस भी विधा में लिखा है, उसमें श्रेष्ठ है।
आलोचना में मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए–रामचंद्र शुक्ल के अलावा नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण साही, नामवर सिंह और मलयज–इनकी आलोचना को ध्यान में कम रखा गया है, लेकिन उनको पढ़ना चाहिए। निर्मल वर्मा ने जो आलोचना लिखी है वो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उपन्यास, कहानी और कविता के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मैंने हंस के एक अंक में उन पर टिप्पणी लिखी है, ‘निर्मल आलोचक।’ कुंवरनारायण द्वारा लिखी आलोचना पढ़नी चाहिए। हमारे यहां जो अकादमिक मुख्यधारा है उसमें इसको स्थान नहीं मिला, वरना अज्ञेय, मुक्तिबोध, विजयदेवनारायण साही, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मलयज, ये जो गैर अध्यापकीय आलोचक हैं, इन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण काम किया है। छायावाद पर नामवर सिंह की एक अच्छी पुस्तक थी, लेकिन छायावाद पर जो दूसरी महत्त्वपूर्ण पुस्तक है, इधर के आलोचकों में वो रमेशचंद्र शाह की है।
? आपने तो कई पत्रिकाएं निकाली हैं। एक अच्छी पत्रिका में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे मित्र विद्यानिवास मिश्र ने एक पत्रिका निकाली–साहित्य अमृत। अभी भी निकलती है। उसकी दो विशेषताएं हैं, एक कि वो धारावाहिक है। यानी वो कभी बंद नहीं हुई। दूसरा ये कि वो कभी अच्छी भी नहीं हुई। उसके बड़े–बड़े संपादक हुए, एलएम सिंघवी, त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी। जब उसका लोकार्पण हो रहा था तो मुझे भी बुलाया गया था बोलने के लिए। मैंने उसमें कहा कि हो सके तो पत्रिका नहीं निकालना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप पत्रिका क्यों निकालना चाहते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। आप दृश्य में हस्तक्षेप करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? वो मुकाम जिस पर आप पत्रिका निकाल रहे हैं, वो मुकाम ठीक से लोकेट होना चाहिए।
हमने ‘पूर्वग्रह’ पत्रिका निकाली थी, तो उसके पीछे स्पष्ट अवधारणा यह थी कि हमारे पेशेवर आलोचक समकालीन रचना के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और हमारी अकादमिक आलोचना जड़ हो गई हैं और इस समय सबसे अच्छी आलोचना स्वयं रचनाकार लिख रहे हैं। इसलिए पूर्वग्रह इनकी पत्रिका होगी। यह उसकी मूल दृष्टि थी। उस समय उस हस्तक्षेप का मतलब निकला। इसलिए ये तय होना चाहिए आपके मन में कि आप क्या करना चाहते हैं?
और एक तरह की भावुक और सह्दय उदारता पत्रिका निकालने में मदद नहीं करती कि मतलब आप हर तरह की चीज छापने को तैयार हैं क्योंकि बहुत कूड़ा लिखा जाता है।
तीसरा, उस पत्रिका के कुछ लेखक होने चाहिए, जिन पर आप निर्भर कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपद्धर्म की तरह आपकी मदद करेंगे। मान लीजिए आप चाहते हैं किसी पुस्तक की समीक्षा हो, आपने जिसको दे रखी है, वो नहीं कर पा रहा है और उस लेखक की उस समय पुस्तक समीक्षा निकलना जरूरी है किन्ही भी कारणों से, तो कम से कम कोई आपद्धर्म की तरह निभाने को तैयार हो। तो एक सशक्त समूह होना चाहिए लेखकों का, जो उस पत्रिका से जुड़ा हो और जो अपनी सबसे अच्छी रचना उस पत्रिका को देने के लिए भावात्मक रूप से प्रतिबद्ध हो।
एक पूरा आभासीय जगत पैदा हो गया है। हर जगह कूड़ा होता है तो इसमें भी कूड़ा है, लेकिन कुछ–कुछ अच्छा भी है, कभी–कभी अच्छी कविता निकल आती है। कभी कोई अच्छी बात कहता है, तो कोई एक ऐसा तरीका निकलना चाहिए, जिसमें कोई अच्छी चीजें उसमें आ रही हैं तो उनको लोक लिया जाए और छाप दिया जाए।
देखिए, ‘पूर्वग्रह’ की कीर्ति या दुष्कीर्ति जो भी थी, उसमें यह महत्त्वपूर्ण था कि किस महत्त्वपूर्ण पुस्तक की समीक्षा जा रही है और ये भी काबिलेगौर होता था कि किस पुस्तक की नहीं जा रही है। आपकी कीर्ति तो इसी से बनेगी कि आप क्या करते हैं और क्या छोड़ते हैं। फिर यह कि पत्रिका किसको संबोधित है।
वामपंथी लोग बहुत पत्रिकाएं निकालते हैं और बहुत मोटी–मोटी निकालते हैं, असह्य रूप से मोटी और भयानक रूप से संकीर्ण, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ अच्छा भी छपता ही है। उनकी दृष्टि यह है कि हमको अपनी दृष्टि का प्रचार करना है लेकिन उस दृष्टि के तले वो ऐसा भी कर जाते हैं कि संभवत: पहले जमाने में ऐसा नहीं हो सकता था, जब ज्यादा संकीर्णता थी। वो सहधर्मियों को संबोधित पत्रिकाएं हैं। मतलब जो उनकी विचारधारा में विश्वास करता है और जो उनके आसपास है।
हिंदी में व्यापक पाठक को संबोधित कोई पत्रिका लगभग है ही नहीं। फिर एक सजग पाठक तैयार करना पत्रिका का कर्तव्य होना चाहिए। यानी एक संवेदनशील सजग पाठक और बहुलतावादी पाठक। ऐसा पाठक, अपनी दृष्टि उसकी जो भी है बनी रहे, इस पर कोई आपत्ति नहीं, किसी की कोई दृष्टि है तो है लेकिन वो दृष्टि दूसरी दृष्टियों से संवाद के लिए खुली दृष्टि हो। वो पाठक होगा सजग। हम अपनी दृष्टि में एकांगीपन से लगे हुए हैं, तो हमारी दृष्टि का हमारे अलावा किसी के लिए कोई उपयोग नहीं है। उससे कोई संवाद संभव नहीं होगा, संवाद तो तभी संभव है जब आप खुले हों।
जब दृष्टि समग्र होने का दावा करने लग जाए तो उस दृष्टि में विकृति आना अनिवार्य है। जब साम्यवाद को लगा कि संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर उसके पास है, तो उसमें विकृतियां आना शुरू हो गईं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी यही होगा कि हमको तो समग्र भारत की समझ है। अगर ये समग्रता का दावा होने लग जाएं तो फिर वो विकृतियां आएंगी ही, कोई रोक नहीं सकता। तो व्यक्ति की दृष्टि खुली हो क्योंकि संसार में अनेक दृष्टियां हैं और उनमें आपस में संवाद, घमासान, संघर्ष, द्वंद्व सब चलेगा, तनाव, नोक–झोंक ये सब होते रहेंगे। और फिर इस समय एक गंभीरता की जरूरत इसलिए भी है कि सनसनी फैलानेवाले माध्यम बहुत हो गए हैं। और झूठ फैलानेवाले माध्यम भी बहुत हो गए हैं। तो चूंकि ये माध्यम इतने अधिक हो गए हैं, इसलिए पत्रिका को सच पर टिकना चाहिए और सनसनी फैलाने से बचना चाहिए। उसकी टोपी उछाल दी, उसके बारे में कुछ लिख दिया, ये टोपी उछाल–कीचड़ उछाल इससे बचना चाहिए। एक सभ्य पत्रिका निकलना चाहिए, जो पाठक को भी सम्मान से देखें और लेखक को भी सम्मान से देखें।
? हिंदी में कौन–कौन सी ऐसी पत्रिका है जो इस मानक पर खरी रही है?
एक जमाने में कल्पना थी, कृति थी, युगचेतना थी–जो लखनऊ से निकलती थी। सुरूचिपूर्ण पत्रिका थी ज्ञानोदय और नया ज्ञानोदय उन दोनों के बीच में कहीं थी–उसमें भी कुछ सनसनी फैलाने जैसा था। हमारे मित्र रवींद्र कालिया भी सनसनीप्रिय थे। बहरहाल, थोड़ा–बहुत इधर उसमें सुधार हुआ है। चूंकि ‘पहल’ ने अपना पुराना तेवर बदल दिया और अधिक समावेशी हो गई तो उसमें भी अच्छी सामग्री छपती रहती है।
अज्ञेयजी प्रतीक निकालते थे। अच्छी पत्रिका थी। नया प्रतीक उतनी अच्छी नहीं बन पाई। क्योंकि तब तक समय बदल गया था। लेकिन प्रतीक तो प्रतिमान ही है।
हिंदी में तीन पत्रिकाएं कम से कम ऐसी हुई हैं जो अपने समय में प्रतिमान बनी–एक तो ‘सरस्वती’, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जमाने में बहुत प्रतिमान बनी, दूसरी थी ‘प्रतीक’ और तीसरी थी ‘कल्पना’, जो हैदराबाद से निकलती थी और बद्री विशाल पित्ती जिसके संपादक थे। ये तीन पत्रिकाएं प्रतिमान थीं, फिर बाद में ‘कृति’, जो श्रीकांत वर्मा और नरेश मेहता ने निकाली थी।
पुस्तक पत्रिकाएं थीं, जो एक–दो–तीन अंक निकलकर रह गईं। इलाहाबाद से निकली थीं, एक थी–‘नई कविता’, जिसके चार–पांच–छह अंक निकले थे, शायद जगदीश गुप्त और साहीजी संपादित करते थे। और दूसरी एक पुस्तक पत्रिका थी ‘निकष’, जिसे धर्मवीर भारती और ये ही लोग संपादित करते थे। तीसरी थी, उपेन्द्रनाथ अश्क ने निकाली थी–‘संकेत।’ और चौथी थी, ‘हंस’ का एक वार्षिक पुस्तक जैसा अंक निकला था, अमृत राय और बालकृष्ण राव ने निकाला था। एक पुस्तक पत्रिका पटना से भी निकली थी, बहुत अच्छी थी, ‘अपरम्परा।’ संभवत: राजेन्द्र किशोर निकालते थे। पटना में तब राजकमल चौधरी थे। मेरी कुछ प्रेम कविताएं जो थोड़ा अधिक ऐंद्रिक थीं जिसे कल्पना ने वापस कर दी थी, लेकिन उसे राजकमल चौधरी ने छापी थी।
अभी भी ‘तद्भव’ पत्रिका है जो निकलती है लखनऊ से। इलाहाबाद से मार्कण्डेय ने निकाली थी–‘कथा।’ अभी ‘अनहद’ का एक अंक आया है, अच्छा है वो, उसमें नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह आदि के ऊपर काफी सामग्री है। मेरा छोटा भाई संपादित करता है पत्रिका ‘समास’। तो कुल मिलाकर दृश्य इतना खराब नहीं है।
लेकिन इसमें अगर कोई एक नई पत्रिका निकालने की सोचेगा, तो यह विचारणीय है कि आप क्यों एक पत्रिका निकालना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो ये पत्रिकाएं नहीं कर पा रही हैं, जो आप करना चाहेंगे? अच्छे लिखनेवाले दो तरह के लोग होते हैं, एक तो अच्छा अपने आप लिखनेवाले होते हैं। दूसरा, संपादक का एक काम कुछ लोगों से अच्छा लिखवा लेना होता है। अनुनय, विनय, क्रोध फुसला–उसलाकर उनके ऊपर उतारू रहे।
तीसरा, ऐसा सोचना चाहिए कि दुनिया में इस समय कैसी पत्रिकाएं निकल रही हैं। संसार में पत्रिकाएं बहुत हैं। पत्रिकाओं के अलग–अलग रूप हैं।
मैं सोचता हूं कई बार, ऐसी पत्रिका कोई क्यों नहीं निकालता, जिसमें वो तय करे कि पैंतीस वर्ष की आयु के नीचे के युवाओं की ही रचनाएं छापेंगे, इससे ऊपर का हम छापेंगे नहीं। पैंतीस या चालीस जो भी आयु आप तय कर लें। उसमें बुजुर्ग यदि कोई होगा भी तो वो बुजुर्ग होगा जो किसी युवा पर लिखेगा, इस तरह से आप कुछ बुजुर्गों को समकालीन लेखन से जोड़े भी रखेंगे।
मैं उन्नीस बरस का था, जब रघुवीर सहाय की पहली पुस्तक ‘सीढि़यों पर धूप में’ प्रकाशित हुई। 1959–60 में। मैं बीए करके यहां आया था एमए करने। श्रीकांतजी ने मुझसे कहा कि तुमको रिव्यू करना है ‘कृति’ के लिए। वैसे मैं एक–दो रिव्यू पहले ‘कल्पना’ में अजित कुमार और एकाध और की कर चुका था लेकिन मैंने ये रिव्यू कुछ ज्यादा ध्यान देकर की। उसी के थोड़े दिन बाद एक–दो बरस बाद ‘62–63 में देवीशंकर अवस्थी ने तय किया कि वो कुछ पुस्तक समीक्षाओं का एक संचयन तैयार करे। उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम्हारी कौन सी समीक्षा ली जाए। मैंने कहा कि ये रघुवीर सहाय पर लिखी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी राय भी यही है, रघुवीरजी से पूछा था कि आपकी पुस्तक की कौन सी रिव्यू ली जाए तो उन्होंने कहा कि अशोकजी का रिव्यू ले लीजिए।
आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है? एक संपादक जो मुझसे कम से कम दस बरस बड़ा है, मुझसे अपने एक समवयसी पर लिखवा रहा है फिर जिस पर मैंने लिखा है वो एक दूसरे समवयसी संपादक से कह रहा है कि इसको शामिल करिए।
कम से कम मेरे हिसाब से इस समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्रफी में, रंगमंच के बारे में मैं उतना नहीं कह सकता, नृत्य के बारे में उतना आवश्स्त नहीं हूं, इनमें पैंतीस की आयु के युवा बहुत काम कर रहे हैं और नए ढंग का काम कर रहे हैं। मतलब नवाचार का युवामंच होना चाहिए उसको। बुजुर्गों के लिए बहुत सारी और जगहें हैं, वे वहां जाएं और लिखें।
? सबसे बड़ा साहित्यकार पिछले पचहत्तर साल में किसे माना जाए, इस बारे में आपका कोई मत बना है?
एक बताना बहुत मुश्किल है। और बहुलतावादी के लिए तो ऐसे ही मुश्किल है। क्योंकि वो तो एक में विश्वास ही नहीं करता। मैं कहूंगा हमारे जो सबसे बड़े लेखक हुए हैं वो दस–बारह तो कम से कम हैं–अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर, रेणु, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण साही, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, त्रिलोचन।
? ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञेय हर विधा में श्रेष्ठ हैं।
अज्ञेय के बिना आधुनिक कविता संभव न होती। श्रेष्ठ उपन्यासकार, श्रेष्ठ कहानीकार, श्रेष्ठ संपादक, श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ आलोचक, श्रेष्ठ डायरी लेखक तो वे हैं ही।
? अज्ञेय के बारे में मार्क्सवादियों ने इतना भ्रम फैलाया है लेकिन फिर भी अपने लेखन के दम पर वे शीर्ष पर हैं।
इसलिए मैं तो एक तरह से अपने को अज्ञेय की राह पर चलनेवाला मान सकता हूं। निर्मल वर्मा पर पहली आलोचनात्मक पुस्तक का संपादन मैंने किया था, जो 1990 में शायद निकली है, जिनमें वे सब लेख छपे हैं जो ‘पूर्वग्रह’ में आए थे। एक ऐसी दूसरी पत्रिका कोई नहीं हैं जिसमें इतनी सारी सामग्री हो, जिसे पुस्तकाकार निकाली जा सके। शायद ‘आलोचना’ होगी, अगर होगी तो। बाकी और कोई पत्रिका नहीं है। चार–पांच तो हम निकाल ही चुके। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, निर्मल वर्मा पर, अब हो जाएगी मुक्तिबोध पर। रघुवीर सहाय पर हो सकती है, श्रीकांत वर्मा पर हो सकती है। नामवर सिंह पर हो सकती है, सबसे ज्यादा तो ये हमारे यहां छपे थे।
? साहित्यिक लेखन की दुनिया में कोई आना चाहता है तो इसके लिए उसे किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए?
मैं कई बार यह कहता रहा हूं कि जब आप एक कविता लिखना चाहें तो उसके पहले आपने सौ कविताएं पढ़ रखी हों। मतलब यह कि आपको पता हो कि भाषा में क्या हो चुका है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई भाव है जो आपको बहुत ईमानदारी से और बड़ी शिद्दत के साथ अभिभूत कर रहा है। आप चाहते हैं कि आप उसको लिखें। हो सकता है उस भाव को पहले किसी कवि ने बेहतर ढंग से कह रखा हो। प्रेम पर कालिदास ने भी लिखा। तो कालिदास की प्रेम–कविता से मेरी प्रेम–कविता को अलग होना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी।
कुमार गंधर्व से हमने कहा कि आप कालिदास को गाइए। कालिदास समारोह होता था उज्जैन में। मैं उसका कर्ता–धर्ता था। मैं यह आग्रह चार–पांच वर्ष करता रहा। वे हां, हां करते रहे। एक बार मैंने कुछ ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने कहा–ये बताओ, मैं गाऊं न गाऊं, कालिदास महान् कवि हैं? हमने कहा–हां, हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं न गाऊं तो उनकी महानता में कोई कमी आएगी? हमने कहा–नहीं, नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तभी गाऊंगा जब मेरे गाने से उनकी महानता में कोई अंतर आता हो, यानी मैं उसको या तो बढ़ाता होऊंगा या उसको सत्यापित करता होऊंगा। अगर वो उससे स्वतंत्र महान् है तो मेरे गाने से क्या फायदा?
हमारी नई पीढ़ी की बड़ी भारी समस्या है कि इससे ज्यादा कम–पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी पहले नहीं हुई है। हमलोग भी युवा थे। हम तो छोटे शहर में युवा थे। अब छोटा शहर कौन छोटा रह गया! सब शहरों में बहुत सारी सुविधाएं एक जैसी हो गई हैं।
हमने उन्नीस वर्ष की उम्र में काफ्का को पढ़ लिया, रिल्के को पढ़ लिया, नेरूदा को पढ़ लिया, पाज को पढ़ लिया, नाजिम हिकमत को पढ़ लिया, इतने सारे लोगों को पढ़ लिया था। आप दिल्ली में बैठे हैं, पटना, लखनऊ, बनारस या जयपुर में बैठे हैं, जहां अधिक साधन हैं, अधिक पुस्तकें हैं, अधिक बड़े पुस्तकालय हैं। आपकी जिज्ञासा ही नहीं जागती। विश्व कविता का इतना अनुवाद किया गया है, जिसे अभी तीन वॉल्यूम में ‘तनाव’ नाम की पत्रिका के सारे पचास–पचपन कवि छापे हैं, लेकिन उसके प्रति कोई जिज्ञासा युवाओं में नहीं है। इतनी आत्मरत–आत्मकेंद्रित कम पढ़ी–लिखी पीढ़ी, ये ज्यादा चलती नहीं है।
टीएस इलियट ने कहा था, पच्चीस बरस की उम्र तक तो हर आदमी अपने को कवि समझता है और कविता लिखता है, वही कवि विचारणीय है जो पच्चीस साल के बाद भी कविता लिखे। इसका एक उदाहरण यह भी था अगर पच्चीस साल तक कोई मार्क्सवादी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो विचारणीय नहीं है लेकिन पच्चीस साल के बाद भी मार्क्सवादी है तब भी वो विचारणीय नहीं है।