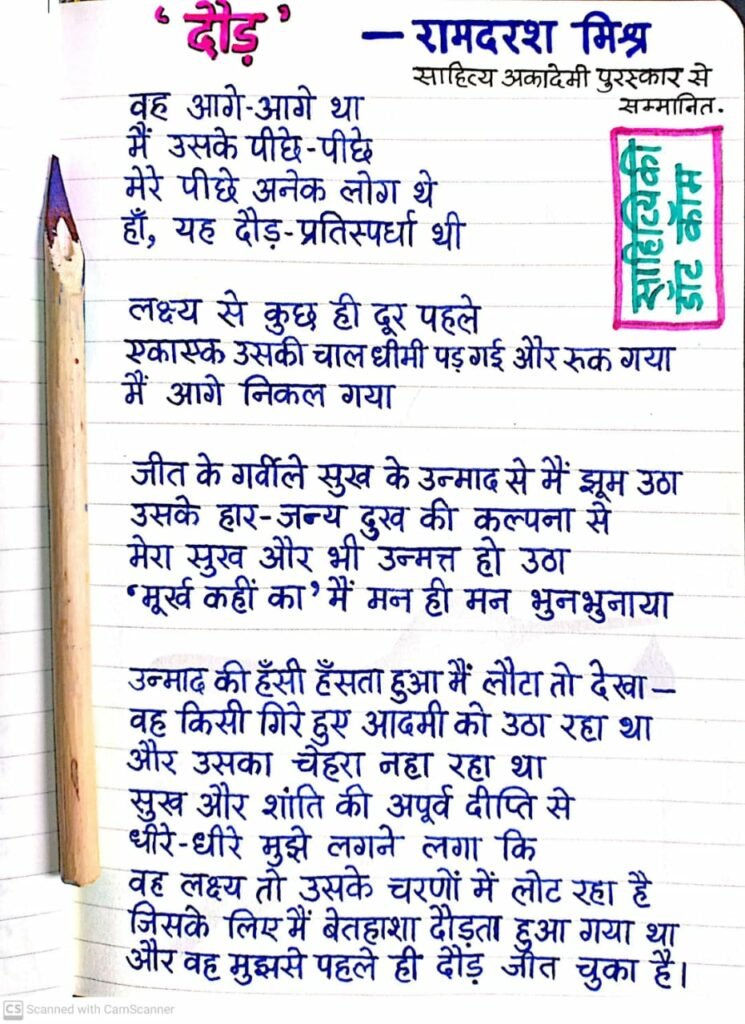कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप बेचैन हो जाते हैं और आपके मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ‘जूठन’ एक ऐसी ही आत्मकथा है। वाल्मीकि जी की कविता ‘ठाकुर का कुआँ’ मैंने सोशल मीडिया साइट्स पर पढ़ी थी। वहीं से इच्छा हुई उनके बारे में और जानने की और उनकी लिखी कहानियाँ, कविता, निबंध आदि पढ़ने की। ‘जूठन’ उनकी आत्मकथा है और शायद उनकी लिखी किताबों में सबसे प्रचलित भी। ‘जूठन’ को अगर मैं अपने जीवन में अभी तक पढ़ी हुई आत्मकथाओं में से सबसे असरदार आत्मकथा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप बेचैन हो जाते हैं और आपके मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ‘जूठन’ एक ऐसी ही आत्मकथा है। वाल्मीकि जी की कविता ‘ठाकुर का कुआँ’ मैंने सोशल मीडिया साइट्स पर पढ़ी थी। वहीं से इच्छा हुई उनके बारे में और जानने की और उनकी लिखी कहानियाँ, कविता, निबंध आदि पढ़ने की। ‘जूठन’ उनकी आत्मकथा है और शायद उनकी लिखी किताबों में सबसे प्रचलित भी। ‘जूठन’ को अगर मैं अपने जीवन में अभी तक पढ़ी हुई आत्मकथाओं में से सबसे असरदार आत्मकथा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
‘जूठन’ मूलतः ओमप्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन के हर पहलू को पाठक के सामने उजागर करती है। शुरुआत उनके बचपन से होती है, बरला गाँव (मुज़फ़्फ़रनगर जिला, उत्तर प्रदेश) जो मूलतः सवर्ण जाति के लोगों की वजह से जाना जाता था। गाँव में ऊँची जाति के लोग वर्णव्यवस्था ज्यों की त्यों बनाए रखने के लिए ‘चुहेड़ी’ (वाल्मीकि जी इसी जाति से आते हैं) को बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे। बंधुआ मजदूरी, उत्पीड़न, शोषण और न जाने कितनी सामाजिक कुरीतियाँ जो ग्रामीण जीवन का अभिशाप थी। वाल्मीकि जी के पिताजी की एक बात बहुत प्रभाव डालती है, “पढ़ लिख कर जाति सुधारो”, शायद इन्हीं शब्दों से हिम्मत पाकर अनेक अत्याचार और यातनाएँ सहकर भी वाल्मीकि जी पढ़ते रहे।
हाईस्कूल में वाल्मीकि जी को रसायनशास्त्र के प्रैक्टिकल में जानबूझ कर फेल किया जाता है, निराश होकर आगे की पढ़ाई करने वे अपने मामा के यहाँ देहरादून चले जाते हैं। यहाँ जाति का दंश जरा कम लगता है, भेदभाव होता है लेकिन फिर भी गाँव से काफी बेहतर हालत थी। यहाँ एक पुस्तकालय में पहली बार वाल्मीकि जी का परिचय डॉ. भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व, साहित्य और दर्शन से होता है, उनके लिए यह एक नव चेतना जैसी चीज़ थी। देहरादून में विषम गरीबी और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी जैसे-तैसे वो अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखते हैं। यहाँ वाल्मीकि जी के बहुत से घनिष्ट मित्र भी बनते हैं और उनकी साहित्यिक प्रतिभा भी निखरती है। यहीं से वे आर्डिनेंस फैक्टरी में शामिल होने की परीक्षा देते हैं और फिर जबलपुर चले जाते हैं।
यहीं से शुरुआत होती है वाल्मीकि जी के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की। जबलपुर के होस्टल के माहौल में छुआछूत और जातीय भेदभाव कम होता है पर कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे थे जो अभी भी पुरानी लकीर के फकीर थे। जबलपुर से वाल्मीकि जी अम्बरनाथ, महाराष्ट्र पहुँच जाते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। महाराष्ट्र की भूमि महात्मा फुले और डॉ. अम्बेडकर की कर्मभूमि थी। यहाँ दलित चेतना पहले से ही काफी जागृत थी। अम्बरनाथ में वाल्मीकि जी को एक लेखक, रंगकर्मी और कवि के रूप में प्रसिद्धि मिलती है। दफ्तर और बाहर बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हर कदम पर उनका सहयोग करते हैं, सुख-दु:ख में साथ निभाते हैं और बिना उनकी जाति आदि के बारे में पूछते हुए परिवार के सदस्यों जैसा बर्ताव करते हैं।
लेकिन, ऐसा नहीं था कि उनको यहाँ किसी भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ा। दफ्तर में ऐसे बहुत से वरिष्ठ अधिकारी हुए, जो सामंती विचारधारा से ग्रसित थे और यह मानते थे कि एक दलित अधिकारी या कर्मचारी बिना योग्यता सिर्फ आरक्षण के बल पर ही इस मकाम तक पहुँच सकता है। कई बार वाल्मीकि जी का तबादला ऐसे विभागों में हुआ जहाँ जाने के योग्य वे बिल्कुल नहीं थे लेकिन कभी ना जाने वाली ‘जाति’ का बोझ वे यहाँ भी उठा रहे थे। साहित्य सृजन और रंगमंच के लिहाज से वाल्मीकि जी के लिए ये एक सुनहरा समय होता है। यहाँ वे एक नाट्य मंडली की भी स्थापना करते हैं। व्यक्तिगत कारणों की वजह से वाल्मीकि जी अम्बरनाथ से वापस देहरादून आ जाते हैं।
शुरू में वो अपने सास-ससुर के साथ रहकर घर खोजते हैं, पर देहरादून में स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। मकान मालिक सबसे पहले किरायेदार की जाति पूछते हैं और जैसे ही पता चलता है कि वाल्मीकि जी दलित समाज से हैं, घर देने से मना कर दिया जाता है। यह दकियानूसी सोच ही है, जहाँ एक महान साहित्यकार और कलम के सिपाही का केवल उनकी जाति के आधार पर मूल्यांकन होता है। जैसे-तैसे एक घर मिलता है और यहाँ रहते हुए वाल्मीकि जी बहुत सी बेहतरीन कविता, कहानी, नाटक आदि लिखते हैं। उनकी रचनाएँ बहुत सी दलित पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती हैं। उनकी कुछ रचनाएँ हंस कथा मासिक के लिए भी चुनी जाती हैं और वे सीधा राजेंद्र यादव (हंस के संपादक) के संपर्क में भी आते हैं। देहरादून में रहते हुए वाल्मीकि जी की पहचान एक कर्मठ रंगकर्मी के रूप में भी होती है। यहाँ से उनका तबादला जबलपुर हो जाता है जहाँ वो कार्य क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। यहाँ से वापस वाल्मीकि जी देहरादून आ जाते हैं और सेवानिवृत होकर शिमला में उच्च शिक्षण संस्थान में शोध करने के लिए फ़ेलो नियुक्त होते हैं। पर ईश्वर को भी जाने क्या मंजूर था! कुछ ही दिनों में पता चलता है कि वाल्मीकि जी को पेट में ट्यूमर होता है और इलाज़ के लिए उन्हें फ़ौरन गंगाराम अस्पताल, दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू आदि के बहुत से छात्र, शिक्षकगण और साहित्यिक जगत के मित्र और प्रशंसक बीमारी के समय दिन-रात वाल्मीकि जी को घेरे रहते हैं। वाल्मीकि जी को आखिरकार लगता है कि उन्होंने अपने साहित्य सृजन के माध्यम से जाने-अनजाने कितने लोगों के जीवन को छुआ है।
ऐसे आरोप लगते हैं कि वाल्मीकि जी सवर्णों के विरोधी थे, मैं ऐसा सोचने और कहने वालों को ये बताना चाहूँगा कि ‘जूठन’ में उन्होंने अपने बहुत से सवर्ण मित्रों की खूब प्रशंसा भी की है। ऐसे मित्र जो देहरादून में वाल्मीकि जी की जाति पूछे जाने पर एक मकान मालिक से दो-दो हाथ करने को भी तैयार हो गए थे। ऐसे मित्र जो सवर्ण और वरिष्ठ अधिकारी होते हुए भी वाल्मीकि जी को ‘भैया जी’ कहकर बुलाते थे। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। वाल्मीकि जी को इस बात का भी दु:ख होता है कि दलित वर्ग के लोग अपना सरनेम छुपाते हैं और खुद की पहचान को गुप्त रखने के भरसक प्रयास करते हैं। वाल्मीकि जी चाहते थे कि दलित समाज के लोग ऐसा कतई न करें और अपने अस्तित्व को स्वीकार करें, मेहनत से पढ़े लिखें, आगे बढ़ें और समाज सुधार करें। धर्म में भी वाल्मीकि जी की कोई आस्था नहीं होती है, वो मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठे रहते हैं और प्रवेश नहीं करते हैं। दलितों में फैले हुए अंधविश्वास और अन्य कुरीतियों पर भी वो कड़ा प्रहार करते हैं।
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह आत्मकथा किसी भी साहित्यप्रेमी के लिए जरूर पढ़ी जानेवाली पुस्तकों में से एक होनी चाहिए। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मेरी बेचैनी कुछ खास कम नहीं हुई है और मैं अभी भी आज के समाज में वर्णव्यवस्था की प्रासंगिकता के बारे में सोच रहा हूँ। आप भी विचार करिए।