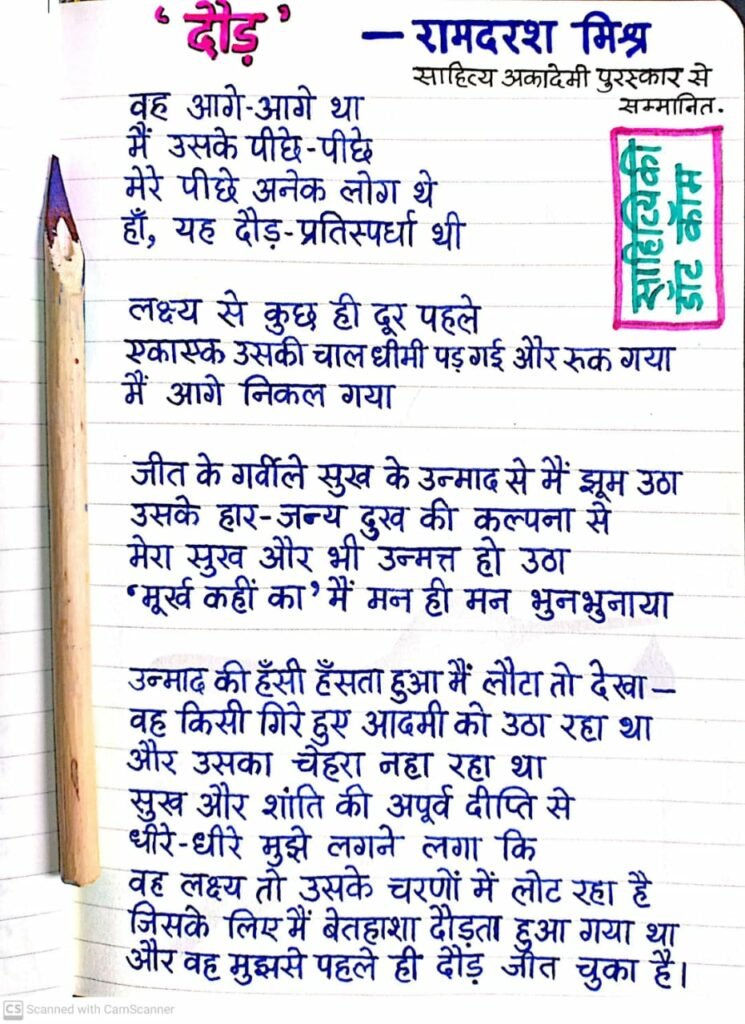“औक़त न क़लम की /न लेखक की/न लेखन की/ज़िन्दगी फैलती चली गई/कागज़ के पन्नों पर/कुछ इस तरह ज्यों धरती में उग आया हो/विशाल जड़ों वाला एक ज़िदा रुख”(कृष्णा सोबती, ‘ज़िंदगीनामा’ के आरम्भ में दी गई पंक्तियाँ)
कहानी के सिरजे गए पात्र जब रचनाकार के जीवन की संचित अनुभूति का परिणाम हों तो निश्चय ही कागज़ के पन्नों पर सायास गढ़े गए चरित्र नहीं असलज़िन्दगियां खुद-ब-खुद फैलती जाती हैं..अनायास। कृष्णा सोबती न सिर्फ हिन्दी कथा जगत बल्कि पूरे विश्व के कथा साहित्य में एक अकेली, अपनी तरह की अनोखी सशक्त कथाकारा हैं। हिन्दी कथा लेखन में जिस तरह के बोल्ड लेखन की शुरुआत उन्होंने की वह स्त्री विमर्श के क्षेत्र का क्रांतिकारी कदम था। उनकी पहचान एक ऐसी लेखिका के रूप में जानी जाती है जो भारतीय स्त्री के अव्यक्त मन की सघन, बहुपरतीय खोह के भीतर मचलते-सुबकते स्पंदन को महसूस कर उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म गांठ को खोल देने का साहस और सामर्थ्य रखती हो। निःसंदेह कृष्णा सोबती का नाम हिन्दी कथाकारों में अग्रणी है।
१९५० में उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई और अभी हाल ही में उनका नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए घोषित किया गया। कह सकते हैं कि ६७ साल की साधना जब किसी पुरस्कार तक पहुंचती है तो उस पुरस्कार की अहमियत बढ़ जाती है। उनका साहित्य हिन्दुस्तानी ज़ुबान का म्यूजियम कहा जाता है। उनकी किसी भी किताब के पन्ने पलट लें,आप उन शब्दों के साथ जीने लगेंगे जो हमारे पुरखे विरासत में छोड़ गए है। ९२ वर्ष की सोबती हिन्दी साहित्य और समाज का चलता फिरता इतिहास हैं। वो हिन्दी की सबसे नौजवान और जुझारू लेखिका हैं। बीते साल बढती असहिष्णुता को लेकर जब चिंतित बौद्धिकों और चिंतकों ने सभा की तो कृष्णा सोबती ने भी विरोध की आवाज़ मुखर कर बाबरी से दादरी के खिलाफ बराबरी की बात की। ये प्रतिरोध किसी दल विशेष के समर्थन या असमर्थन में नहीं था बल्कि उनकी इंसानी और लोकतांत्रिक वैचारिक पक्षधरता का परिणाम था तभी कांग्रेस शासन में भी उन्होंने पद्मविभूषण का प्रस्ताव लौटाया। वो प्रतिरोध की आवाज़ हैं जो लगातार रचनारत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा करते हुए और उन्हें बधाई देते हुए लीलाधर मंडलोई ने कहा कि हिन्दी उर्दू पंजाबी भाषा की लोकशीलता के साथ उन्होंने जो अद्भुत शिल्प, वस्तु और अंतर्वस्तु की शिनाख्त की है वो बेजोड़ है।
हिन्दी साहित्य समाज में जिस आज़ाद औरत की बात की जाती है सोबती ने सम्भवत: उसे सबसे पहले गढ़ा। उनके कथा साहित्य की नायिकाएं जिस जिंदादिली, बेलौस, बेधकड़क अंदाज में अपना जीवन जीती रहीं उसे बाद में कई लेखिकाओं ने अपने किरदारों के लिए अपनाया. अपनी नई किताब ‘गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान’ में वो अपनी ज़िन्दगी के एक हिस्से को उपन्यास में ढालती हैं.उस हिस्से को जब देश बटा था समाज बटा था तहजीब बटी थी और इंसानियत लहू-लुहान होकर कट-छट गयी थी। इस उपन्यास में वे बेहद तकलीफ से लिखती हैं, “अब तो हम तेज़ किए हुए चाकू हैं। हम आग का पलीता हैं। हम दुश्मनों को चाक कर देने वाली गरम हिंसा हैं। हम दुल्हनों की बाँहें काट देने वाले टोके हैं। हम गंडासे हैं। अब हम हम नहीं हैं,हथियार हैं।”
कृष्णा सोबती लगभग एक पूरी सदी जी चुकी हैं ,उनके संस्मरण, आत्मकथात्मक लेख और साक्षात्कार पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई वाचिक इतिहास शुरू हो गया हो। जिस साल भारत गणतन्त्र बना १९५० में ‘लामा’ उनकी पहली कहानी छपी। तब से उनकी कलम चलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सोबती का साहित्य इतिहास द्वारा बेदखल की जा रही मनुष्यता का पक्ष है। मेरे लेख का केंद्र उनका कहानी संग्रह‘बादलों के घेरे’ है, जिसका का प्रकाशन 1980 में हुआ। इसमें २४ छोटी बड़ी रचानाएं हैं। विषय की दृष्टि से इन्हें प्रेम और स्त्री-पुरुष सम्बन्ध से सम्बन्धी, पूरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्त्री की यातना को और उस के परिवेशगत अंतर्द्वंद्व के चित्रण सम्बन्धी और विभाजन की यातना को जीती, लहू-लुहान होती इंसानियत से सम्बन्धी कहानियों की श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। इस संग्रह के कवर पेज पर वे लिखती हैं कि इन कहानियों में एक समय है जो बीत जाने के बाद भी हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है,जो अविस्मरणीय है और उससे कुछ न कुछ हम सीखते हैं और अपने जीवन को आगे बढाने के लिए प्रेरित होते हैं। ये कहानियाँ पाठकों को सम्वेदनाओं के कई धरातलों पर छूती हैं उन्हें झकझोरती और उनका हृदय करुणा और सम्वेदना से भर उठता है. विजय मोहन सिंह इनकी रचनाओं के बारे में ‘बीसवीं शताब्दी का हिन्दी साहित्य’ में लिखते हैं, “ सोबती जी के कथा लेखन की विशेषता समझने के लिए उनका बारीकी से अध्य्यन करना जरूरी है वरना उनकी कहानियों की बनावट इतनी सघन है कि प्राय: आसानी से सरलीकृत निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं।”इस सरलीकृत का ही नतीजा है कि आलोचक गोपाल राय हिन्दी कहानी का इतिहास -2 में ‘बादलों के घेरे’ कहानी के बरक्स उनकी अन्य कहानियों में ‘याद रखने वाली कोई विशेष बात नहीं’ देखते हैं।
कृष्णा सोबती जिस समय रचना कर्म में पदार्पण करती हैं वह समय न सिर्फ राजनीति, और समाज बल्कि उनके लेखन के दौर के क्रम में साहित्य में भी गहरे बदलाव और उथल-पुथल का दौर था। ‘बादलों के घेरे’ की दो चार कहानियों को छोड़कर बाकी की कहानियों का रचना काल हिन्दी कहानी साहित्य में ‘नई कहानी’ आन्दोलन नाम से जाना जाता है। यह वह समय था जब आज़ादी के बाद का मोहभंग, मूल्य संक्रमण, संयुक्त परिवारों का विघटन, पुरानी पीढ़ी के परिवार में व्यर्थ होते जाने की पीड़ा, स्त्री-पुरुष संबंधों में आता गहरा बदलाव, व्यक्ति स्वातन्त्र्य, अस्तित्व के लिए संघर्ष और स्त्री में आती चेतना जैसे नए बदलाव तेजी से उभर रहे थे। सोबती इस समय को जी रहीं थीं। उनका लेखन इस बदलाव को आत्मसात कर धीरे-धीरे अपनी रौ में बहता है , यहाँ बदलाव की सब कुछ उखाड़ फेंकने की आंधी नहीं। ये सच है कि प्रेम सम्बन्धों को लेकर इस संग्रह की कहानियां उनके उपन्यासों के बरअक्स रोमानी और भावुक हैं। “बावजूद ,इस तथ्य को नए सिरे से उद्घाटित करतीं हैं कि तन का धर्म मन के धर्म से अलग नहीं होता। नई कहानी आन्दोलन के दौर में जैनेन्द्र और अज्ञेय की मनोवैज्ञानिक कहानियों के विरुद्ध काफी कुछ लिखा गया। कृष्णा सोबती उसी परिवर्तित दृष्टि को रचनात्मक स्तर व्यक्त करती हैं।”(मधुरेश,हिन्दी कहानी का विकास,पृष्ठ103) इस जगह वे अपने दौर के अमूमन कहानी लेखकों से अलगभी पड़ती दिखती हैं जहाँ उनके समकालीन लेखक स्त्री-पुरुष रिश्तों में अहम की गुंजलकों में उलझे थे, वे प्रेम और सिर्फ प्रेम को तरजीह देती हैं। वे प्रेम से भरे स्त्री-पुरुष विशेषकर स्त्री के मन की अतल गहराइयों को गहरे नापने की कोशिश करती हैं।यहाँ वे नई कहानी आन्दोलन के मूल स्वर ‘भोगे हुए यथार्थ’ के स्थान पर समाज में मौजूद चलते-फिरते पात्रों की कहानियाँ कहने का प्रयास करती हैं। उन्होंने जटिल यथार्थ को कहानी में रचा, फिर चाहे क्यों न उस पर आदर्श और रुमान के आरोप लगे हों।
‘बादलों के घेरे’, ‘कुछ नहीं-कोई नहीं’, ‘एक दिन’, ‘पहाड़ों के साए तले’ और ‘दो राहें :दो बाँहें’ जैसी कहानियां अलग-अलग तरीके से एक ही भाव को कैनवस पर अलग-अलग रंगों से उकेरती हैं ये भाव है स्त्री-पुरुष का अह्मरहित, निज रहित अटूट सान्द्र प्रेम। ‘बादलों के घेरे’ में व्याप्त स्वार्थरहित निश्छल प्रेम की सघनता और गहरी सम्वेदना के सन्दर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, “जो कहानी सम्वेदनात्मक तीव्रता की दृष्टि से मन को छूती है, और बार-बार पढ़कर भी बासी नहीं लगती, वह कहानी है : ‘बादलों के घेरे’। इस कहानी में प्रेम की जानमारू संवेदना का, क्षय रोग से ग्रस्त,मृत्यु की प्रतीक्षा करते व्यक्ति के रीतते प्राणों कीघुटन और अकेलापन का, अपनों के पराए हो जाने की विवशता का दुर्लभ अंकन हुआ है।प्रेम की सम्वेदना का अंकन इतने संकेतात्मक, पर प्रभावी रूप में हुआ है कि उससे गुजरते हुए सिहरन हो जाती है।…इस कहानी में भाषा अपनी सर्जनात्मकता के शिखर पर पहुंची हुई है और उससे संवेदना मानो टपकती हुई प्रतीत होती है।”(हिन्दी कहानी का इतिहास-2 पृष्ठ ६६-६७)
‘कुछ नहीं-कोई नहीं’ में पर-पुरुष के प्रेम में पड़ी विवाहित स्त्री के मन के द्वंद बेहद बारीकी से उजागर हुए हैं। पति रूप के मित्र आनन्द के प्रति शिवा के अंजाने आकर्षण और समर्पण के बाद पति की ठंडी और कठोर प्रतिक्रिया उसे घर छोडकर आनन्द के साथ जाने को विवश कर देती है। किन्तु वह कभी भी आनन्द के साथ रूप की पत्नी की तरह स्वाभिमान और अधिकार से नहीं रह पाती। बच्चों के लिए वह दूसरी माँ है, जो जिम्मेदार है उनके पिता को उनसे अलग करने के लिए, समाज की दृष्टि में ‘दूसरी औरत’ के भाव के अपराध बोध से ग्रस्त शिवा के पास अपने निर्णय पर पछताने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। उसकी नियति इतनी कठोर है कि आनन्द की मृत्यु हो जाती है, घर और उसकी प्रापर्टी पर उसका कोई हक नहीं इसलिए उसे घर से बाहर जाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया जाता है। अंतत: अपने निर्णय के कारण शिवा एकाकी, अपराध बोध से ग्रस्त जीवन बिताने पर विवश है। वहीं ‘एक दिन’ में दो स्त्रियाँ एक पुरुष की पत्नी बनकर उसकी प्रेम की दया पर निर्भर हैं,यही उनकी नियति है। धर्मपाल पत्नी शीला के होते हुए भी दूसरी स्त्री श्यामा को घर में पत्नी की तरह रखता है। शीला की पीड़ा, श्यामा के भीतर का असुरक्षा का भाव और धर्मपाल का उनके भाग्य विधाता के रूप में दोनों तरफ डांवाडोल मन; स्त्री के कोमल मन, पति रूपी पुरुष के प्रति पूर्ण समर्पण, समाज भीरुता , पति के प्रति स्वामी भाव और निष्ठा को व्यक्त करता है। पहली कहानी जहां ‘समाज में प्रेम के अनाम सम्बन्ध की अपेक्षा वैवाहिक जीवन का प्रेम ही अंतत: सत्य है’ का दर्शन , वहीं दूसरी कहानी पति के व्यभिचारी, अनैतिक, अमर्यादित रूप को शीला द्वारा क्षमा कर, मायके गयी श्यामा के कारण पति के कुछ दिनों के खैरात में मिले प्रेम को पुन: अपनाकर अपना भाग्य सराहना; समाज में पुरुष शोषित व्यवस्था का चित्रण है। ये दोनों कहानियाँ ’५२, से , ‘५५ के समय की हैं। विजयमोहन सिंह की यदि मानें तो इन्हें तत्कालीन समय का दस्तावेज़ समझ आदर्श प्रेम, आदर्श समाज, वैवाहिक संस्था की आदर्श परिकल्पना की कहानियां समझना इनका सरलीकृत निष्कर्ष होगा। तो क्या ६० के दशक में ‘मित्रो मरजानी’ की मित्रो जैसी कद्दावर पात्र रचने वाली सोबती इन कहानियों के रूप में पुरुषपोषक व्यवस्था का पोषण कर रही थीं? मेरी समझ में ऐसा नहीं है। वो शिवा, श्यामा, और शीला जैसे स्त्री पात्रों के माध्यम से अपने समय को रच रहीं थीं। ये वो स्त्रियाँ हैं जिनका मानसिक अनुकूलन पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा किया गया है। ये अनुकूलन ही स्त्री शोषण की जड़ है। स्त्री का द्वंद और तनाव, झटके से रिश्तों को तोड़ न पाने की कशमकश ; यह शुरुवात थी उस प्रतिरोध की जो आगे जाकर मित्रो की आवाज़ बनती है। यहीं से आगे चलकर सोबती के पात्र जीवन के तमाम निषेधों, वर्जनाओं, द्वन्द्वों और अपराधबोध को तोड़कर बाहर आ सके।
इस संग्रह की कहानियों की कालावधि १९४४ से १९६० तक की है। जिसमें ‘नफ़ीसा’ जैसी डेढ़ पृष्ठ की छोटी सी कहानी से लेकर २० पृष्ठ तक की ‘बादलों के घेरे’ जैसी लम्बी कहानियां हैं। उनके कथा साहित्य का फलक विस्तृत है। इनकी ‘मित्रो मरजानी’, ‘ तिन पहाड़’, ‘यारों के यार’ जैसी रचनाएं उन दिनों कहानी के रूप में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपीं बाद में उन्हें उपन्यास का रूप दिया गया। इनकी कहानियों में व्याप्त मांसलता और बोल्डनेस को लेकर विभिन्न आलोचकों ने समय-समय पर अपना विवाद, ऐतराज जाहिर किया क्योंकि जिस तरह के लेखन का साहस वो कर सकीं उनके दौर की सम्भवत; ही कोई लेखिका कर सकी. ‘बादलों के घेरे’ में उनकी लम्बी कथा-यात्रा को समेटती चौबीस कहानियां हैं। इनमें उनकी एकदम आरम्भिक दौर की कहानियों में ‘नफ़ीसा’ और ‘लामा’ सन १९४४ की हैं। डेढ़ पृष्ठ की कहानी ‘नफ़ीसा’ और दो-सवा दो पृष्ठ की कहानी ‘लामा’ बालमन की बेहतरीन कहानियां हैं, जहां मृत्यु के अर्थ और उसके भय से बचपन नावाकिफ़ है। छोटी सी कहानी ‘नफ़ीसा’ एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो अपने परिवार से अलग अस्पताल में अपने नजदीक आती मृत्यु से अंजान,अपने परिवार और वहां बीतते दिनों की याद में तरसती है, हंसती है फिर खेलती है।उसकी मासूमियत,और उसके बचपन को निगलता काल कितना निर्मम और क्रूर है, वो नहीं जानती। छोटी सी कहानी में सम्वेदना का अंतर्व्याप्त सघन रूप चमत्कृत करता है , “वह जीवन का मोल नहीं जानती,मौत को भी नहीं पहचानती। उसकी आँखों में भोलापन है, सिर्फ भोलापन! उसे न बीमारी का खौफ़ है ,न मौत का डर। वह तो जानती है खिलौने, गुड़िया,मोटर,तांगा, अम्मी और अब्बा नूरी और इकबाल।” इसी तरह बचपन के खेल में जीवन को झकझोर देने वाली अप्रत्याशित घटना के बालमन पर प्रभाव को लेकर लिखी गयी कहानी ‘टीलो ही टीलो’ है।
‘बदली बरस गई’, ‘आज़ादी शम्मोजान की’ और ‘गुलाबजल गंडेरियाँ’ कहानियाँ स्त्री की अतीव पीड़ा और यातना को उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंकित करने वाली कहानियां हैं। इनमें किसी भी प्रकार का निषेध या वर्जनाएं नहीं है, न ही भावुकता और रोमान। बदली बरस गई पति की मृत्यु के बाद ससुराल में यातना और घरेलू हिंसा की शिकार स्त्री का गुरु की शरण में जाना और वहां जाकर सांसारिक मोह माया से दूर होकर साध्वी माता बनने की कोशिश में युवा होती बेटी का सामाजिक मोह का चित्रण बेहद रोमांचक है। माँ ने समस्याओं से पलायन कर लिया लेकिन उसकी बेटी सामाजिक मोह माया से जबरन मुंह नहीं मोड़ सकती। वह उसी घर में पुन: जाने का फैसला लेती है जो उसकी माँ छोड़ कर आई थी। ‘आज़ादी शम्मोजान की’ बेहद मार्मिकता से देह व्यापार में संलिप्त स्त्रियों की पीड़ा को उकेरती है। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है लेकिन शम्मोजान के लिए आज़ादी का मतलब बेमानी है, बेमतलब है। यहाँ कमलेश्वर की कहानी ‘माँस का दरिया’ याद आती है। देह व्यापार की वीभत्सता और कुरूपता उनके तन और मन दोनों को छलनी कर देती है साथ ही इस कहानी में लेखिका एक प्रश्न और उठाती है देह की आज़ादी का, ‘मुन्नी ने अपनी कसी और तंग कमीज में से जरा लम्बी सांस लेकर कहा,“क्या कहा,आज़ादी? लोगों को आज मिल रही है आज़ादी! आज़ादी तो हमारे पास है। हम –सा आज़ाद कौन होगा,शम्मोजान ?”…अपने अंदर ढंके पर्दों को उघाड़कर अगर वह भी देखे,तो एक टूटी आहत छाया उसकी उनींदी आँखों से झलक जाएगी। सालों बीते जब शम्मोजान लाज-शर्म छोड़कर पहली बार इन दीवारों के अन्दर बैठकर मुस्करा दी थी कि अब वह आज़ाद है। जिस आज़ादी को अभी-अभी मुन्नी ने अपनी बेसुरी आवाज़ में याद किया था, वह आज कितनी विकृत और कितनी कुरूप हो चुकी है,यह आज उसे भूला नहीं।’‘दादी अम्मा’, ‘अभी उसी दिन ही तो’ कहानियां परिवारों में अधिकार छीन जाने के बाद सास और दादी बन जाने वाली स्त्रियों के आहत अभिमान की मार्मिक गाथा है। ये कहानियाँ चरमराते संयुक्त परिवारों की कहानियां हैं।
विभाजन की त्रासदी की मारक और प्रामाणिक कहानियाँ ‘सिक्का बदल गया’, ‘मेरी माँ कहाँ ..,’ ‘डरो मत,मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा’हैं। इस सन्दर्भ में वे कहती हैं कि , “विभाजन एक ऐसे ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन है याद रखना खतरनाक।”(कृष्णा सोबती, सोबती-वैद सम्वाद, लेखन और लेखक) ‘मेरी माँ कहाँ..’की दहशत मंटो की इस थीम पर लिखी कहानियों की याद दिलाती है। सोबती की इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है, दोनों कौमों में व्याप्त नफरत, हिंसा, डर, अविश्वास और इन सबके बीच छलनी होती मानवता के बीच से ही फूटता इंसानियत का छोटा सा उत्स। ये उनका भरोसा था जो कायम रहा।
कृष्णा सोबती की कहानियों और उपन्यासों की एक अन्य बड़ी विशेषता है उनकी भाषा। जो उन्हें बाकी अन्य लेखकों से विशिष्ट बनाती है। वह कहती हैं, “भाषा सिर्फ वो नहीं जिसे हम लिखित में पढ़ते-लिखते हैं, संवाद में बोलते हैं, भाषा वह भी है जिसे हम जीते हैं।”( सोबती-वैद संवाद)
वस्तुत: कृष्णा सोबती की कहानियों में जीवन की चेतना है। ये कहानियां उनके समय और परिवेश का व्यापक वितान हैं, बल्कि इन्हें लगभग आधी शताब्दी का दस्तावेज़ कहा जा सकता हैं। ये कहानियां सोद्देश्यता को लेकर नहीं रची गईं बल्कि ये उनके रचनात्मक ,सजग लेखक मन की उपज हैं जो अपने समय को शब्दों का जामा पहनाकर खुद ब खुद सार्थक रूप लेती गयी। सोबती मानती हैं कि,‘वो ऐसे ही लिखने के लिए नहीं बैठ पातीं जब कोई घटना, वस्तु,विचार आंदोलित करता है, जब वो उसे अपने अंदर आत्मसात करती हैं तब किसी रचना का जन्म होता है. उस कृति के साथ उनका निजी आत्मिक सम्बन्ध बन जाता है।’ ‘नई कहानी’ आन्दोलन में कृष्णा सोबती अकेली कहानीकार हैं जिन्होंने इतनी कम कहानियां लिखकर अपनी विशेष पहचान बनाई है. उनकी प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह बादलों के घेरे सन ८० में प्रकाशित हुआ. अपने कम लिखने के कारणों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है, ‘मुझ में एक गहरा ठंडापन है. कभी-कभार लिखने बैठ ही जाती हूँ तो वह मेरे निकट समूची प्रक्रिया का एक अंग बन जाता है. कुछ भी लिखना मेरे निकट समूची प्रक्रिया का एक अंग बन जाता है. कुछ भी लिखना मेरे निकट एक गम्भीर और जोखिम भरी स्थिति बन जाती है इसीलिए मैं अपने लेखक को कभी पटाती नहीं. दांव पर नहीं लगाती. अपने से हटकर मैं उसे दूसरा व्यक्ति समझती हूँ और उसकी इज्ज़त करती हूँ…(सारिका ,जनवरी ’७९ पृष्ठ 9) ‘नई कहानी के बेहद आत्मपरकता वाले दौर में लेखक और भोक्ता के बीच की यह दूरी किसी हद तक आश्चर्यजनक लग सकती है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा सोबती के अपने अनुभव और आग्रह उनकी कहानियों में न हों,लेकिन उनके जीवन-प्रसंगों में प्रवेश की वैसी छूट नहीं मिलाती जैसी उस दौर के अन्य बहुत से लेखकों के साथ मिलाती है। उनकी कहानियां उनके अनुभवों का ताप संजोए रखकर भी उन्हें आत्मवृत्तांत के रूप में लिए जाने की छूट प्राय: नहीं देती।’(हिन्दी कहानी का विकास , मधुरेश पृष्ठ 102-103) तभी स्त्री विमर्श पर बेहद प्रमाणिक लेखन करने वाली सोबती कहती हैं कि , “लेखन तुक्कों की मार नहीं ,लेखक होना एक पूरी तालीम है। लेखक के पास लेखक का अनुभव संसार है। अपने अंदर की बाहर की स्थितियों को और अपने को पढने की जीवन दृष्टि।” (आजकल पत्रिका में पूर्व प्रकाशित)